देश की सीमाओं की रक्षा करना सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अक्सर सरकार की लोकप्रियता के भिन्न पैमानों में एक यह भी होता है कि उसने सीमाओं की रक्षा किस हद तक की है। यह अलग बात है कि ज़मीन पर सीमा निर्धारण से लेकर उसकी हिफ़ाज़त के तौर-तरीक़ों तक की समझ विकसित करने में सरकारें ही जनता की ‘मदद’ करती हैं। कई बार यह मदद एक ऐसे दुश्चक्र का निर्माण कर देती है जिसमें फँस कर सरकारें सीमा से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण दायित्व को नज़रअंदाज़ करने लगती हैं। वे यह भूल जाती हैं कि जितना महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा है उससे कम अपने पड़ोसियों के साथ चल रहे सीमा विवादों का हल ढूँढना नहीं है।
एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत के सामने सीमा चुनौतियाँ दो काल खंडों में आयीं। पहली तो एक उपनिवेश के रूप में मिली जब दिल्ली पर क़ाबिज़ एक तत्कालीन विश्व ताक़त ने आसपास के कमज़ोर शासकों से अपने अंतरराष्ट्र्रीय हितों को ध्यान में रख कर सीमा समझौते किये। इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण थे।
पहली के अंतर्गत अफ़ग़ानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन खींची गयी और दूसरी तिब्बत तथा भारत के मध्य की मैकमोहन लाइन थी जिसने उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैले हिमालय पर्वत की शृंखलाओं के 3000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र मे फैली सीमाएँ निर्धारित कीं। देश के विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के साथ सीमाएँ तय करने की ज़रूरत पड़ी। पाकिस्तान बन जाने के बाद डूरंड लाइन तो अब भारत के लिये अप्रासंगिक हो गयी है पर इस तथ्य को रेखांकित करना ज़रूरी है कि म्यांमार या बर्मा को छोड़ कर अपने हर पड़ोसी से, जिससे स्थल सीमा मिलती है, हमारे विवाद हैं। आज़ादी के बाद की हमारी सरकारों के लिये क्या यह नहीं कहा जाना चाहिये कि उन्होंने देश की अखंडता की तो बख़ूबी रक्षा की पर पड़ोसियों से सीमा विवादों को हल करने में वे बुरी तरह से असफल रही हैं। यह कहना अहमन्यता होगी कि हमेशा हमारे पड़ोसी ही ग़लत हैं।
गलवान घाटी में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद 6–7 महीनों तक देश के साथ पूरा विश्व दम साधे किसी अनहोनी की आशंका में डूबा रहा था। शून्य से क़ाफी नीचे हाड़ कँपाती ठंड में पचास हज़ार से अधिक भारतीय सैनिक लगभग इतने ही चीनी सैनिकों की आँखों में आँखें डालकर महीनों खड़े रहे। असावधानी से भी चली एक गोली दो परमाणु बम संपन्न और दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले इन पड़ोसियों के साथ हमारी दुनिया को महाविनाश की विभीषिका में झोंक सकती थी। ग़नीमत ही कही जा सकती है कि उभय पक्षों को सदबुद्धि आयी और दोनों ने पीछे हटने का फ़ैसला किया।
पर एक अवकाश प्राप्त फौज़ी अफ़सर के अनुसार अगर यह समझौता सिर्फ़ एक छोटे से क्षेत्र के लिये है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, यह सार्थक तभी होगा जब इसे विस्तार देते हुए पूरी भारत–चीन सीमा तक ले ज़ाया जाए।
भारत–चीन सीमा विवाद के हल की कामना करने के पहले हमें उसे समझना होगा। इस विवाद की जड़ में मैकमोहन लाइन है जो 1914 में भारत तिब्बत (और चीन) के प्रतिनिधियों के बीच शिमला में हुए एक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आयी थी। इस सीमा रेखा की भारतीय और चीनी समझ में अंतर के फलस्वरूप ही विवाद होते हैं और यही बिगड़ने पर सशस्त्र संघर्षों का रूप ले लेते हैं। मैकमोहन लाइन को पवित्र मानने के पहले हमें दो तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो यह कि समझौता दो असमान शक्तियों के बीच हुआ था– मेज़ के एक तरफ़ तत्कालीन विश्व की सबसे ताक़तवर ब्रिटिश हुकूमत बैठी थी जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और दूसरी तरफ़ हर तरह से कमज़ोर तिब्बत था। एक तीसरा पक्ष भी था जो दूसरे की ही तरह कमज़ोर था और यह चीन था जिस का प्रतिनिधि वार्तालाप के दौरान बिना दस्तख़त किये ही भाग गया। इस समझौते को चीन ने आज़ाद होने के बाद कभी मंज़ूर नहीं किया और हमेशा एक ताक़तवर द्वारा हाथ मरोड़ कर कराया गया माना।
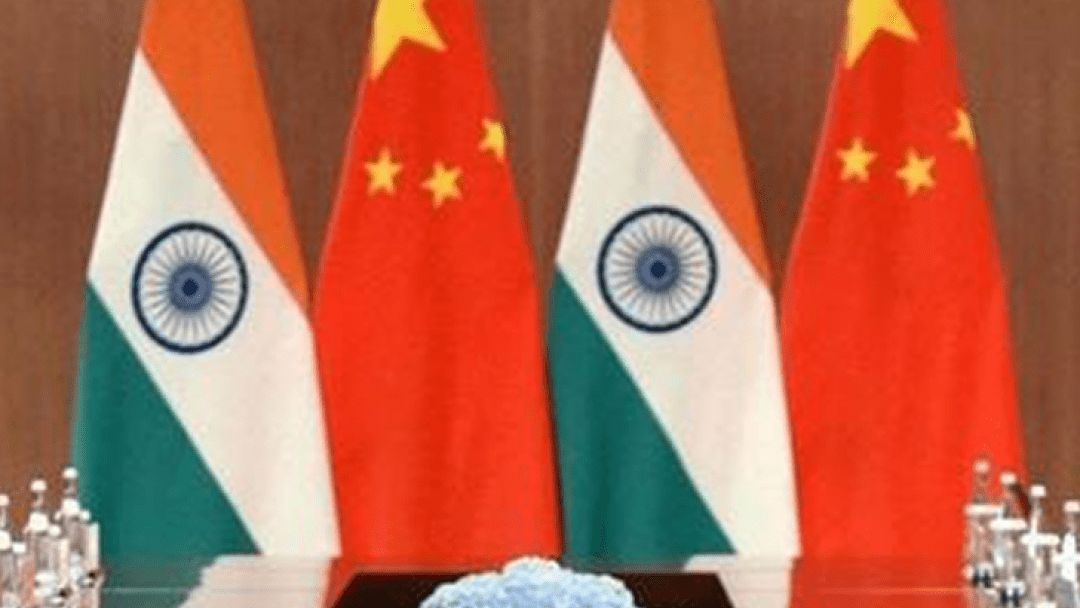
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1949 के बाद दोनों देश मैकमोहन लाइन पर लचीला रुख़ अपना कर कई बार स्थाई समझौते तक पहुँच चुके हैं और हर बार अंध राष्ट्रवाद की आँधी चलाकर नासमझ राजनैतिक शक्तियों ने इसे असंभव बना दिया है। 1959 में चीनी प्रधानमंत्री चाउएनलाई की दिल्ली यात्रा के विवरण उपलब्ध हैं जिनके मुताबिक़ वे नई दिल्ली में एक प्रस्ताव के साथ निर्णय लेने वाले केंद्रीय मंत्रियों की कोठियों पर भटकते रहे। एक महत्वपूर्ण मंत्री ने तो उनसे मिलने से ही इंकार कर दिया। दूसरे ताक़तवर मंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू को शौचालय के अंदर से ही जवाब दे दिया कि उन्हें चाउएनलाई के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिये।
क्या देश की जनता को यह जान कर धक्का नहीं लगेगा कि आज जिस आधार पर भारतीय और चीनी सेनाओं ने अपने को पीछे किया है वह तो वही है जिसका प्रस्ताव 1959 में चीन ने दिया था?
एक वीडियो कार्यक्रम में ले. जनरल (रिटायर्ड) एच. एस. पनाग ने इस तथ्य को उजागर किया है। उनके अनुसार सेना मुख्यालय में टंगे नक़्शों में इस इलाक़े को ‘चीन द्वारा दावा किया गया क्षेत्र’ दर्शाया गया है। इसी इंटरव्यू में जनरल पनाग ने यह भी कहा कि भारत सामरिक रूप से इतना मज़बूत तो है कि चीन को किसी बड़ी विजय से रोक सके पर यह दावा कि वह एक साथ दो मोर्चों (अर्थात पाकिस्तान और चीन) पर लड़ सकता है, वास्तविकता से कोसों दूर है। जिस कार्यक्रम में जनरल पनाग इन तथ्यों को बता रहे थे उसमें एक दूसरे रिटायर्ड ले. जनरल डी. एस. हुडा भी मौजूद थे और उनकी खामोशी इन दावों पर मुहर लगा रही थी।
राष्ट्र प्रेम एक उदात्त भावना है पर अंध राष्ट्रवाद हमें आत्महत्या के लिये प्रेरित कर सकता है। जब जवाहर लाल नेहरू ने आक्साई चिन के लिये कहा कि वहाँ तो घास का एक तिनका नहीं उगता तो उन्हें कांग्रेस के ही एक सांसद का व्यंग्य सुनना पड़ा कि उनके सिर पर भी बाल नहीं हैं तो क्या उसे भी दुश्मन को सौंप दिया जाए? 1962 की शर्मनाक हार का देश के मनोबल पर क्या असर पड़ा, हमें कभी भूलना नहीं चाहिये। बजाय इतिहास को दोहराते हुए सरकार को युद्ध के लिए कूद पड़ने को मजबूर करने के हमें उसे याद दिलाते रहना होगा कि उसके लिये जितना ज़रूरी सीमाओं की हिफ़ाज़त करना है उससे कम ज़रूरी सीमा विवादों को हल करना नहीं है। थोड़ा लचीला रुख़ अपना कर इसे हासिल किया जा सकता है पर इसके लिये जनता को अंधराष्ट्रवाद की भूलभुलैया से बाहर निकालना होगा।
(साभार - हिंदुस्तान)
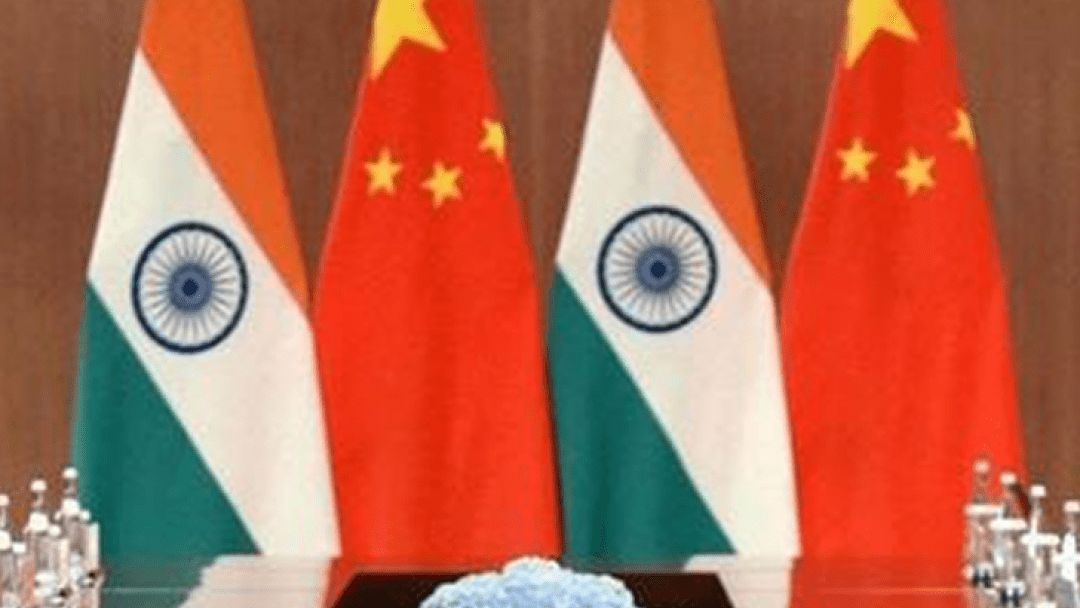

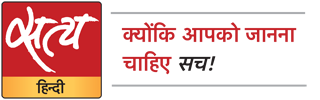





























अपनी राय बतायें