सन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन ने महात्मा गाँधी को भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन का खेवनहार बन जाने का अवसर प्रदान किया था। यह वही किसान आंदोलन था जिसकी कोख से जन्मा सत्याग्रह भविष्य के नागरिक अवज्ञा आंदोलन का मुख्य औज़ार बना। ऐसा औज़ार, जिसने आने वाले दशकों में ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला कर रख दी थीं। क्या दिल्ली के बॉर्डर पर जन्म लेने वाले किसान धरने भी इक्कीसवीं सदी के चम्पारण में विकसित होने की दिशा में है? क्या यह धरना भी बीजेपी की घराना पूंजीवाद की राजनीति के ऊपर चढ़े हिन्दूवाद के मुलम्मे की चूलें हिला कर रख देने की तैयारी कर रहा है?
गाँधी के स्वराज की विशेषता थी। आसमान में लहराता इसका ध्वज आंदोलन की राजनीति के रंग में जितना रंगा-पुता था, आंदोलन की संस्कृति में उतनी ही रची-बसी थीं उसकी जड़ें। सिंघु, टिकड़ी और गाज़ीपुर के बॉर्डरों पर इन दिनों आंदोलन की राजनीति के साथ-साथ आंदोलन की जैसी संस्कृति दिखायी दे रही है, आज़ादी के बाद के किसी आंदोलन में दिखायी नहीं दी। तो क्या यह मान लेना उचित होगा कि इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक दिल्ली सीमांत पर किसी एक व्यक्ति या नेतृत्व के एक समूह को गाँधी के रूप में जन्म देने की तैयारी कर रहा है?
बीसवीं सदी के दूसरे दशक में पहुँचे गाँधी ने नील खेतिहरों के दमन और शोषण के विरुद्ध राजनीति का बिगुल बजाकर सोते हुए अंग्रेज़ हुक्मरानों को जगा दिया था। औपनिवेशिक कृषि समाज में राजनीतिक चेतना के ये नए स्वर थे, भविष्य में समूचा देश जिनसे एकाकार हुआ। दक्षिण अफ्रीका के अपने छोटे-मोटे अनुभवों से गाँधी जान गए थे कि औपनिवेशिक समाज में प्रतिरोध की स्वतंत्र राजनीति तभी स्थाई हो सकती है जब इसके समानांतर स्वतंत्र संस्कृति भी विकसित की जाए। चंपारण के अपने प्रारंभिक अध्ययन में उन्होंने महसूस किया कि इस निरक्षर और अर्द्ध शिक्षित ग्रामीण भारतीय समाज में शिक्षा की कितनी अहम आवश्यकता है। 1917 में उन्होंने 3 स्कूलों की आधारशिला रखी। पहला मोतिहारी में, दूसरा भितिहरवा में और तीसरा मधुबन में।
शिक्षा और काम के बीच के गैप को भरने के लिए उन्होंने कई सारे 'बुनियादी' स्कूलों की स्थापना की जिनमें कताई, बुनकरी, कारपेंटरी और खेती का प्रशिक्षण दिया जाता था। राजनीतिक आंदोलन के समानान्तर यह एक नए प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने न सिर्फ़ इलाक़े के निर्धन किसानों और खेतिहर मज़दूरों को जागरूक किया बल्कि नयी राजनीति का नेतृत्व सँभालने की दिशा में गाँधी स्वयं भी प्रशिक्षित हुए।
उधर इलाक़े के वकीलों, शिक्षकों और दूसरे मध्यवर्ग में अपने प्रति बढ़ती जागरूकता और चेतना से गाँधी ने यह भांप लिया था कि साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन अकेले किसानों के दम पर नहीं जीता जा सकता है, इसके साथ मध्यवर्ग की सहभागिता भी ज़रूरी होगी। उन्होंने प्रारंभिक रूप से अपने स्कूली अभियान में शिक्षा के प्रसारक के तौर पर इस वर्ग को जोड़ा। बाद में यही वर्ग उनकी राजनीतिक शक्ति भी बने।
चंपारण के इन्हीं राजनीतिक-सांस्कृतिक 'सूक्ष्मतर' अनुभवों को गाँधी ने आगे चलकर समूचे देश पर लागू किया और सफलता हासिल की।
गाँधी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जिन आश्रमों की स्थापना की, वे उनकी इसी राजनीतिक-सांस्कृतिक विचारधारा के सम्मिलन के प्रशिक्षण केंद्र थे जिसका प्रारम्भिक अनुभव उन्हें चंपारण में हुआ था। ये आश्रम वस्तुतः तत्कालीन औपनिवेशिक-सामंती भारतीय समाज के बीच में एक अलग प्रकार की नागरी सभ्यता के दीप सरीखे थे। 1921 में मीराबेन को लिखे पत्र में उन्होंने स्वीकार किया ‘चंपारण के अनुभवों ने मुझे पूरे देश को समझने का अवसर दिया।’

जून में जब मोदी सरकार ने गुपचुप रूप से नए कृषि क़ानून सम्बन्धी अध्यादेश को लागू किया और पंजाब में इसके विरोध में आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ तो मोदी शासन ने आदतन इसे बहुत हल्के में लिया। उसने एक ओर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया तो दूसरी ओर मालवाहक रेलगाड़ियों की आवाजाही को आंदोलन के बहाने से रोक दिया। ऐसा करके वे पंजाब के शहरी मध्यवर्ग को किसानों और अमरेंदर सिंह के ख़िलाफ़ भड़का कर बीजेपी की पैठ का विस्तार चाहते थे। पाँचवें महीने जब किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया तो मोदी एंड कम्पनी तब भी उन्हें बहुत हल्के में आँकती रही। मनोहरलाल खट्टर और उनकी हरियाणा सरकार ने हाइवे खोद कर और पीडब्ल्यूडी विभाग के गोदामों से भारी भरकम बोल्डर निकल कर सड़कों पर बिछा देने, आँसू गैस छोड़ने और वाटर कैनन से भिगो देने मात्र से समझ लिया कि वे आंदोलनकारी किसानों की राह का रोड़ा बनने में कामयाब होंगे। पंजाब के किसान इन बाधाओं को कूदते-फाँदते आख़िरकार दिल्ली आ पहुँचे। उनके साथ हरियाणा के किसान तो एकजुट होने ही लगे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वे किसान भी स्वयंस्फूर्त रूप से आने लग गए जिनके नेतृत्व में बैठे टिकैत आदि के बारे में यह आम अवधारणा थी कि उन्हें रोक पाने में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का क्षेत्रीय दबाव काम कर जाएगा।
दिल्ली पहुँचने वाले किसान जत्थों पर शुरू में बीजेपी नेतृत्व और उनके आईटी सेल ने 'खालिस्तानी', 'पाकिस्तानी', 'माओवादी', 'अल्ट्रा लेफ्ट' आदि-आदि के नारों से उन पर हमला बोले लेकिन उनके इन प्रहारों का कोई ख़ास असर नहीं हुआ।
दिल्ली की सरज़मीं पर पहुँचकर पंजाब के किसान नेतृत्व ने अपने आंदोलन की राजनीति के साथ-साथ आंदोलन की संस्कृति का भी रंग बिखेर दिया। नेतृत्वकारी पंजाब के किसानों के दिल्ली पहुँचने का राजनीतिक और सांस्कृतिक रंग आहिस्ता-आहिस्ता पूरे देश में बिखरने लग गया। आज हालत यह है कि पूरे देश का किसान पंजाब के किसान आंदोलन के पीछे कतारबंद होने लग गया है।

उन्होंने अपनी यह रणनीति प्रत्यक्षतः गाँधी से सीखी या नहीं लेकिन इतना तय है कि उन्होंने गाँधी सरीखे राजनीतिक और सांस्कृतिक सत्याग्रह को दिल्ली की धरती पर बो दिया। आज़ादी के बाद के युग में 'दिल्ली चलो' का आह्वान बहुत बार हुआ है लेकिन दिल्ली पहुँचकर वे यहाँ स्थायी भाव से जम नहीं गए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आंदोलनकारियों ने दिल्ली के भीतर अपना समानांतर शहर बसाया हो और न समानांतर नागरी सभ्यता और संस्कृति की स्थापना की हो। गाँधी युग के बाद ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि इन किसानों का साथ देने के लिए पंजाब (और कालांतर में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) के खेतिहर मज़दूरों के अलावा स्थानीय आढ़तिया, छोटा दुकानदार, कृषि औज़ारों के निर्माता, शिक्षक, लेखक, कवि, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, फ़िल्म निर्माता, अभिनेता और स्क्रिप्ट लेखकों का जमावड़ा-संक्षेप में समूचा मध्यवर्ग आंदोलन की परिधि के भीतर उनके पक्षधर की हैसियत से आ गया।
जिस तरह भारत सहित सारी दुनिया में चर्चित पंजाबी के नामचीन गायकों और संगीतकारों ने इन दिनों दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर डेरा जमा लिया है। वहाँ मौजूद लाखों किसानों की मुश्किलों से भरी ज़िंदगी के पक्ष में बने गीतों को वे सब गा रहे हैं। भारतीय किसानों का दर्द और उनके लूट और शोषण को बेताब बीजेपी सरकार और घराना पूंजीपतियों के षड्यंत्रों का दर्द उनके गीतों के ज़रिये वीडियो, ऑडियो- नेट और यूट्यूब पर सारी दुनिया के करोड़ों भारतीयों और दूसरी नस्लों के बीच जगह पा रहे हैं। कला और हंसिया की ऐसी जुगलबंदी हमेशा नये इतिहास को जन्म देती आई है। ऐसा इतिहास जिसने हर बार राजसिंहासन को डांवाडोल किया है।
क्रान्तिकारी बिरसा मुंडा की खोज का श्रेय देश के मशहूर मानव विज्ञानी (एंथ्रोपॉलॉजिस्ट) कुमार सुरेश सिंह को जाता है। आईएएस के बिहार कैडर में चयन के बाद प्रोबेशन पीरियड में सिंह की पहली नियुक्ति एसडीएम- खूँटी (अब झारखण्ड) में हुई। डाक बंगले में रुके युवा अधिकारी ने रात में दूर से समवेत स्वर में आते गीतों को सुना। अगले दिन उन्होंने मुंडा जनजाति के अपने चौकीदार से जब पड़ताल की तो पता चला कि ये ‘बिरसा भगवान’ के गीत हैं। सुरेश सिंह ने अपनी कई महीनों की खोज में जो नतीजे हासिल किए वे चौंका देने वाले थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़े गए जनजातियों के युद्ध का समूचा इतिहास इन गीतों में था। कुमार सुरेश सिंह ने इन्हें क्रमवार संकलित करके उस समूचे इतिहास को विस्तार में खड़ा किया जिसे अंग्रेज़ इतिहासकारों ने एक-दो लाइन में निबटा दिया था।

उनकी किताब 'द डस्ट-स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट' दुनिया में बिरसा मुंडा के इतिहास का पहला प्रामाणिक दस्तावेज़ है। वे सारे गीत न सिर्फ़ इस इतिहास पुस्तक का आधार हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि उक्त महान संघर्ष के पार्श्व में गीत और संगीत का कैसा अमिट योगदान रहा है। बांग्ला की सुप्रसिद्ध रचनाकार महाश्वेता देवी का 'साहित्य अकादमी' से पुरस्कृत उपन्यास 'आरण्येर अधिकार' (जंगल के दावेदार) कुमार सुरेश सिंह की इसी पुस्तक पर आधारित और उन्हें समर्पित है।
हॉवर्ड फ़ास्ट 20वीं सदी के अमेरिका के प्रख्यात यहूदी उपन्यासकार थे। 1951 में प्रकाशित उनका उपन्यास 'स्पार्टाकस' रोम साम्राज्य में ईसा से 73 साल पहले हुए ग़ुलाम विद्रोह पर आधारित है जिसका नेतृत्व स्पार्टाकस नामक ग़ुलाम ने किया था। 'उपन्यास' में विसूवियस पर्वत शृंखला की विशाल शिलाखण्डों पर तराशे गए भव्य स्मारकों का उल्लेख है, ग़ुलाम मूर्तिकारों ने विद्रोह युद्ध के दरमियान जिनका निर्माण किया था। स्मारक में उकेरे गए 50 फिट ऊँचे एक ग़ुलाम की मूर्ति का ज़िक्र करते हुए रोमन सेनापति क्रैसस अपने दोस्तों से कहता है ‘वह पैर फैला कर खड़ा था। उसकी ज़ंजीर टूट गई थी और आस-पास ही झूल रही थी। एक बाँह में वह बच्चे को उठाए, छाती से चिपकाए हुए था और दूसरे हाथ में एक स्पेनी तलवार थी। ...हाथ के पट्टे और ज़ंजीर की रगड़ से पैदा हुए ज़ख्म तक उसके पाँव में नख्श कर दिए गए थे।’ एक ऐतिहासिक जंग के समानांतर कला के अद्भुत निर्माण की कहानी है यह।
टीवी के अपने 'कॉमेडी शो' के छिछोरेपन के लिए प्रख्यात कपिल शर्मा तक ने 'किसान आंदोलन' के पक्ष में बड़ा गंभीर बयान दिया है। उन्होंने सरकार के किसान विरोधी रवैये की कस कर निंदा की है।
कँवर ग्रेवाल, बब्बू मान, हर्फ़ चीमा, हिम्मत संधू, दिलजीत दोसांझ, सोनिया मान, गुरलेज़ अख़्तर, हरजीत हरमन... पद्मश्री प्राप्त सुरजीत पात्र जैसे दर्जनों कवि-साहित्यकार, ये सब बहुत बड़े नाम हैं। ऐसे नाम जो भारत से निकल कर समूचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यूरोप, कनाडा और अमेरिका के करोड़ों दर्शकों के बीच लोक गीतों, सूफ़ियाना गायकी और गंभीर कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक के पंजाबी झंडे बुलंद करते रहे हैं, आज दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हैं। वे नए युग के संगीत का निर्माण कर रहे हैं। वे स्पार्टाकस और बिरसा युग के कलाकारों की स्मृतियाँ जीवंत कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर इन दिनों पंजाब-हरियाणा के उन अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नामचीन खिलाड़ियों के जमघट भी बने हुए हैं जो इन किसानों के पक्ष में अपने राष्ट्रीय पुरस्कारों को लौटा रहे हैं।

किसानों का शहर!
बीजेपी की सरकारें पुराने शहरों पर नया साइनबोर्ड लगाकर ही उन्हें नया शहर मानने की अभ्यस्त हैं लेकिन आंदोलनकारी किसान इस मेट्रो की छाती पर नए कृषक शहरों को आबाद कर रहे हैं। टेंटों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आबाद किसानों के ये शहर दिल्ली के स्वार्थमय और गलाकाट महानगर सहित सारे देश को बता रहे हैं कि हम आंदोलनकारी किसानों के बीच कैसा प्रेम, और सांस्कृतिक भाईचारा और शहादत व क़ुर्बानी का भाव और राजनीतिक समझ के सम्बन्ध हैं। गाज़ीपुर के बॉर्डर पर मुज़फ्फरनगर जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों से आए वे राम और रहीम एक साथ लंगर 'चख' रहे हैं जिन्हें गंदी राजनीति कल तक एक-दूसरे के ख़ून का स्वाद चखने को मजबूर करती थी। सांप्रदायिक संस्कृति को चकनाचूर करके किसानी लूट के विरोध के आंदोलन की कोख से निकली यह साझा संस्कृति है।
इसमें क्या संदेह कि संघर्ष पंजाब की सांस्कृतिक विरासत है। दूसरी सहस्त्राब्दी के पूर्वार्द्ध से ही वे केंद्रीय एशिया से आने वाले हमलावरों और लुटेरों से लड़ते-भिड़ते रहे हैं। यह पंजाब ही था जो हमेशा दिल्ली की मुग़ल हुकूमत को 'चैलेंज' देता रहा।
'जंग सयाल' के संपादक बांकेलाल के लिखे गीत 'पगड़ी संभाल जट्टा' ने 20वीं सदी के पहले दशक के पंजाब को ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया था। पंजाब की मिट्टी ने ही सरदार अजित सिंह, लाला लाजपत राय, घसीटाराम और सूफ़ी अम्बाप्रसाद जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया। यहीं से शहीद भगत सिंह और उनकी विरासत का जन्म हुआ। आज 'पगड़ी संभाल जट्टा' की जगह बीर सिंह के गीत 'हक्कां दी जंग है वीरो सब्रा नाल लड़नी पैनी' (यह अधिकारों का युद्ध है वीरो हम धैर्य के साथ लड़ेंगे) ने ले ली है। संघर्ष की नई संस्कृति देश को दिशा देने की तैयारी में दिखती है।
अपने हृदय में प्रत्येक आंदोलन को चुटकियों में मसल डालने का मिथक पालने वाली मोदी सरकार के लिए पहली बार दिक़्क़त पैदा करने वाली स्थिति नहीं पैदा हुई है। इससे पहले शाहीनबाग़ के 'समान नागरिकता आंदोलन' को भी वे धार्मिक उन्माद की लपटों में झुलसाने निकले थे लेकिन कामयाब न हो सकी और दिल्ली विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हार गई। मोदी सरकार कोरोना के उदय को भले ही वे अपने लिए सौभाग्यशाली मानती हो कि शाहीनबाग़ से पिंड छूटा। यद्यपि न तो अभी 'सीएए' का सवाल गर्भ में सिमट गया है और न शाहीनबाग़ मरुस्थल बन गया है। वह अभी भी उसके गले में कांटे की मानिंद अटका हुआ है। किसान आंदोलन लेकिन निःसंदेह 'सीएए' से बड़ा काँटा है। ऐसा काँटा जो सिर्फ़ मोदी सरकार के गले तक ही नहीं अटका रहेगा बल्कि उसको राजनीतिक हृदयाघात भी दे सकता है।

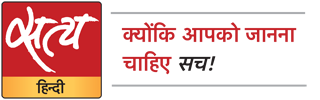















अपनी राय बतायें