‘लोकतंत्र’ इस शब्द को बोलते हुये ही नहीं, इस को जीने की तमन्ना की थी तब जब हमारी पीढ़ी जन्म ले रही थी और हमारे माता-पिता की पीढ़ी अंग्रेजों के शासन की मार से विकल किसी तरह राहत की आशा में हाथ पाँव मार रही थी। आदमी के मरने से पहले आशा नहीं मरती और जब तक आशा नहीं मरती संघर्ष घुटने नहीं टेकता क्योंकि जीवित अवस्था में साहस जितना होता है संघर्ष उतना ही सघन होता जाता है।
मैं कहना यह चाहती हूँ कि गोरों की राजनीति और शासननीति के आमने सामने हम भारतीयों का संघर्ष कई कई रूपों में प्रकट हुआ। उनमें से जो रूप मुख्य था वह आन्दोलन था, सत्याग्रह था, अनशन था और उपवास था। सेना लेकर मार काट की लड़ाई नहीं थी। यह शासक का सामना करने और चुनौती देने का नया रूप था। लेकिन शासक तो शासक होता है, यह जो शान्तिपूर्वक संघर्ष का रास्ता था, अंग्रेजों को बहुत बेचैन करने लगा, इसको फ़तह कैसे किया जाये? साहब बहादुरों के सलाहकारों में बेचैनी बढ़ने लगी, अंग्रेज़ी निज़ाम में खलबली मच गयी।
इसके बाद की घटनाओं को हमारे बुजुर्गों ने देखा है और हमने सुना है कि हमारे देश में अंग्रेज़ी शासकों को आज़ादी के दीवानों का शान्तिपूर्ण संघर्ष तहस नहस करने के लिये हथियार उठाने पड़े और उन्होंने जलियाँवाला बाग जैसे खूनी संग्रामों को अपनाया निहत्थों पर गोलियाँ बरसाईं। मगर जान पर खेलते हुये हमारे उस समय के बूढ़े और जवानों ने जेलों की कालकोठरियों का भय नहीं माना और देश की आज़ादी पर क़ुर्बान होने में कोताही नहीं की। अब यह सब इतिहास है, हम ऐसा मान सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इतिहास अपने आप में जीवित गाथा होती है।
यह सब मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिये कि इस दमन और क़ुर्बानियों के इतिहास में से ही आज़ादी का जन्म हुआ। और यह भी मान लीजिए कि आज़ादी का जन्म होना केवल यहाँ से अंग्रेजों का शासन हटकर उनका जाना भर नहीं था।
सच्ची आज़ादी का मतलब था हमारा अपना भारतीय संविधान बनना और देश के लिये उसका लागू होना जिसकी परिभाषा है - लोकतंत्र = जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिये संविधान। यानी सब कुछ भारतीय निवासियों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिये हो।
भारतीय निवासी भारत के नागरिक के रूप में अपने मत से देश की सरकार चुनेंगे जो सरकार नागरिकों और देश की सीमाओं के हित को ध्यान में रखते हुये काम करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश के नागरिकों को नकारात्मक निर्णयों का विरोध करने का अधिकार भी संविधान देता है क्योंकि संविधान के अनुसार हर नागरिक को बराबरी का अधिकार प्राप्त है यही लोकतंत्र कहलाता है और यही सच्चे मायनों में स्वतंत्रता का रूप है।

हमारे सामने कई ऐसी स्थितियाँ आई हैं जब हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्षीण होते जाने के लक्षण दिखाई दिये हैं। यानी नागरिकों के अधिकारों में कटौती करने की कोशिश में चुनी हुई सरकार अपने फ़ैसले मुक़र्रर करने का एलान करने लगी है। बस ऐसे ही मौक़ों पर नागरिकों की चेतना जागी है और लोगों ने सरकार के ख़िलाफ़ बग़ावत कर दी है। जो बग़ावत लोगों के हितों को बचाने के लिये हो वह लोकतंत्र का हिस्सा है। ऐसी बग़ावतों के उदाहरण दिये जा सकते हैं और हम लोग उन आन्दोलनों से वाक़िफ़ भी हैं। तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुश्मन है। इमरजेंसी के समय को लोग इसी रूप में याद करते हैं। बाबरी मसजिद के ध्वंस को भी लोकतंत्र के ख़िलाफ़ मानते हैं। ऐसे उदाहरण देते हुये आज के समय को देखें तो आज भी of the people, for the people and by the people का धूमिल पड़ते जाना निरन्तर जारी है। जनता कहाँ है और चुने हुये सदस्य गण कहाँ हैं? ये दोनों अपनी-अपनी जगह तो हैं लेकिन अपनी-अपनी भूमिकाओं में नहीं दिखाई दे रहे।
सरकारी नीतियों में खामियाँ
सरकारी नीतियाँ अपने नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिये नहीं उनको कमज़ोर करने पर कमर कस चुकी हैं। हमने जब इमरजेंसी देखी थी तब अपने लोकतंत्र के लिये जेल भरने से नहीं कतराये थे लेकिन जब नोटबन्दी हुई तो बैंकों के सामने अपने हाथ बांधकर खड़े हो गये। कहाँ गुम हो गये विरोध के स्वर? क्या हुआ बग़ावत का जज़्बा? जब जीएसटी लगी तो भी चुप्पी नहीं टूटी। क्या-क्या बताये, बताने पर आयें तो आकाओं के हज़ारों करम याद आने लगते हैं और आँखों के सामने से मज़दूरों की पैदल क़तारें तपती दोपहरी और जलती सड़क से गुजरती दिखती हैं।
सैकड़ों हज़ारों मीलों तक जिनके लिये इस देश में कोई नेता वाहन नहीं दे सका। रास्तों पर मौत नाचती रही, चुने हुये आका लोग तमाशा देखते रहे। रोने वाले देशवासी रोते रहे कि राज्य के शहंशाह उन हारे-थके-बीमार और मौत से लड़ते मज़दूरों को उनके अपने ही घर में नहीं घुसने दे रहे।
इसे हम लोकतंत्र कहें या नहीं? लानत तो हम नागरिकों पर ही भेजी जाये कि हम अपने मत की दृढ़ता में ऐसे दुर्बल होते जा रहे हैं कि रोटी के चंद टुकड़ों और कपड़ों के नाम पर चीथड़ों में लिपटने की एवज़ हमने उन्हीं को सिंहासन सौंप दिया जो मज़दूरों को देश निकाले से गुज़ार रहे थे। किसी देश में तानाशाही चलाने से पहले उस देश के नागरिकों को तबाह कर डालना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर इसमें शक कैसा कि आज देश का किसान कड़े क़ानूनों की आहट पाकर चौकन्ना हो बैठा। यह रबी की फ़सल का मौसम है, किसान के अन्न धन के दिन हैं मगर किसान कहता है कि यही सरकार बहादुर के काले क़ानूनों के दिन हैं जो हमारी मेहनत और फ़सल हड़प जायेंगे।

लोकतांत्रिक अधिकारों के चलते अगर किसान वोट देता है तो अपनी बात कहने का अधिकार भी रखता है मगर उसके अधिकारों को कुचलने का सरकारी फ़रमान उसके सिर पर मंडराता ही रहता है तो वह इस व्यवस्था को कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था माने?
किसान हो या मज़दूर दोनों ही व्यापारियों के सामने अपने आप को असमर्थ और कमज़ोर पा रहे हैं। शेष जनता की बात क्या पूछते हो, भेड़ों के रेवड़ जैसी है, झुंड में चल देती है, भेड़ियों के विरोध में नहीं, भेड़ियों के पीछे-पीछे अपनी ख़ैर मनाती हुई कि जब तक बचें तब तक ही सही।
और यह सच लगता है कि अब समाज में दलित-शोषित और वंचित जैसी जनसंख्या अलग से नहीं, नेता-मंत्रियों और सांसदों-विधायकों जैसे नगीनों को छोड़कर सारी जनता दीन-हीन अवस्था में जा रही है क्योंकि उसका धन और बल लूट लिया गया है! लुटे हुये लोग अपनी विपदा में of the people, for the people and by the people का लोकतांत्रिक सिद्धांत भूल जाते हैं। वे खुद को तानाशाहों के मातहतों के अलावा क्या समझें? विरोध करने की बात मन में आती भी है तो अपने विरोध को बग़ावत के नाम पर जुर्म साबित होने की दहशत घेरने लगती है। मगर डर भय भी कब तक? जब अपना सब कुछ ही लूटा जा रहा है तो अब अपने पास विरोध के सिवा बचा ही क्या है? बेशक जुल्म के ख़िलाफ़ विद्रोह भी तो लोकतांत्रिक मुहिम है।

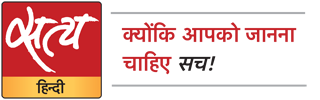














अपनी राय बतायें