यूपी के विकास दुबे एनकाउंटर और उससे पहले तमिलनाडु में पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत के मामले ने पुलिस को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। पुलिस के कामकाज और उसके चरित्र को लेकर बहस छिड़ गई है।
तमिलनाडु में जहां पुलिस का वहशीपन सामने आया, वहीं विकास दुबे प्रकरण में वह बेहद लिजलिजी दिखी। वह इसमें जिस तरह चकरघिन्नी खाती रही उससे पुलिस-अपराधी और राजनेताओं का एक घिनौना गठजोड़ बुरी तरीके से उजागर हुआ। देश की पुलिस का चरित्र कुल मिलाकर यही है- कमजोर को कुचलना और ताकतवर के आगे दुम हिलाना। ब्रिटिश काल से लेकर आज तक उसकी यही फितरत रही।
पुलिस रिफ़ॉर्म की अवधारणा
इन दोनों घटनाओं ने पुलिस सुधार की तरफ नए सिरे से ध्यान खींचा है। कहा जा रहा है कि मूल समस्या पुलिस का राजनीतिकरण है। अगर पुलिस के कामकाज में सियासी दखल बंद हो जाए, उसे स्वायत्तता दे दी जाए, उसकी नियुक्तियों, ट्रांसफर आदि में सत्तारूढ़ दल का एकाधिकार खत्म कर दिया जाए, उसके संसाधन बढ़ाए जाएं, उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तो पुलिस के चरित्र में सुधार हो जाएगा। पुलिस रिफ़ॉर्म की अवधारणा इसी सोच से प्रेरित है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने इन सब चीजों से जुड़े सुझाव रखे थे जिनकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिशा-निर्देश जारी किए। कहने को तो राज्यों ने पुलिस सुधार लागू कर दिए लेकिन सच यह है कि उन्होंने सुधारों का कबाड़ा ही किया है।
अदालत के आदेशों की अनदेखी
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (सीएचआरआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, केवल 18 राज्यों ने 2006 के बाद नया पुलिस एक्ट पारित किया है जबकि बाकी राज्यों ने सरकारी आदेश/अधिसूचनाएं जारी की हैं, किसी ने भी अदालत के निर्देशों का पूरे तरीके से पालन नहीं किया है। ज्यादातर राज्य सरकारों ने इन निर्देशों की या तो अनदेखी की है या फिर स्पष्ट रूप से मानने से इनकार कर दिया है या फिर निर्देशों की हवा निकाल दी है।
1 - हर राज्य में एक सुरक्षा आयोग का गठन।
2 - डीजीपी, आईजी व अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल दो साल तक सुनिश्चित करना।
3 - आपराधिक जांच एवं अभियोजन के कार्यों को कानून-व्यवस्था के दायित्व से अलग करना।
4 - एक पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन।
रिपोर्ट के मुताबिक़, देश के 29 राज्यों में से 27 में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन पुलिस एक्ट या फिर सरकारी आदेश के जरिए किया गया है। लेकिन आयोग के गठन की प्रक्रिया में कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और त्रिपुरा ने राज्य सुरक्षा आयोग में विपक्ष के नेता को शामिल नहीं किया है जबकि 18 राज्यों में आयोग में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र चयन पैनल का गठन नहीं किया है। वहीं, बिहार, कर्नाटक और पंजाब के राज्य सुरक्षा आयोग में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है।
डीजीपी व दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लेकर जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन सिर्फ नगालैंड द्वारा किया गया। 23 राज्यों ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर जारी कोर्ट के निर्देशों की परवाह नहीं की।
इसी तरह डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल होने के निर्देश का पालन सिर्फ चार राज्यों द्वारा किया गया है वहीं आईजी, डीआईजी, एसपी और एसएचओ को कम से कम दो साल का कार्यकाल दिए जाने के निर्देश का पालन सिर्फ छह राज्यों ने किया है।
आपराधिक जांच एवं अभियोजन के कार्यों को कानून-व्यवस्था के दायित्व से अलग करने का काम 12 राज्यों ने नहीं किया है। उसी तरह पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण के गठन में भी हीला-हवाली नजर आती है।
सत्ता पर पकड़ का औजार है पुलिस
सच्चाई यह है कि राजनीतिक नेतृत्व पुलिस से अपना नियंत्रण खोना नहीं चाहता। पुलिस दरअसल सत्ता पर पकड़ बनाए रखने का एक बड़ा औज़ार है। वह जनाधार को संतुष्ट रखने का भी एक जरिया है। क्या वजह है कि सरकार बदलते ही हर मुख्यमंत्री अपनी जाति का पुलिस तंत्र खड़ा करता है।
जातीय आधार पर नियुक्तियां
डीजीपी से लेकर थाने तक में अपने जातीय जनाधार को ध्यान में रखकर नियुक्ति होती है। इससे जनाधार में यह संदेश दिया जाता है कि अपने लोगों को पावर में हिस्सा दिया जा रहा है। कोशिश होती है कि अगले चुनाव में पुलिस राजनीतिक दल विशेष के लिए अनुकूल भूमिका निभाए। अपने विरोधी दलों को खासकर उसके बाहुबलियों को औकात में रखने के लिए अपने मनमुताबिक पुलिस अधिकारियों का रहना जरूरी माना जाता है। अपने समर्थक अपराधियों को संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है।
ऐसे हालात में भला कौन राजनीतिक दल पुलिस सुधार कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे। इसलिए सुधार की अपेक्षा ही बेईमानी है। कोर्ट का लिहाज करके कागज पर सुधार किए जाते हैं बाकी सब वही चलता रहता है।
पुलिस सुधार के पैरोकार मानकर चलते हैं कि पुलिस बल अपने आप में भ्रष्ट, क्रूर या अमानवीय नहीं है, उसे राजनेता ऐसा बनाते हैं। अगर पुलिस दबाव मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर फ़ैसले करने लगे तो वह वैसी नहीं रहेगी, जैसी आज है। यह बात एक हद तक ही सही है। यह एक आदर्श स्थिति की कल्पना है कि सारे पुलिस अधिकारी सदाशयी, ईमानदार, निष्पक्ष और नियम-कानून के प्रति प्रतिबद्ध होंगे और वे सब कुछ सुधार देंगे।
सच्चाई यह है कि सुधारवादी लोग पुलिस के समाजशास्त्रीय पहलुओं को नहीं देखते। वे पुलिस और समाज के संबंधों की शिनाख्त किए बगैर एक सरल निष्कर्ष निकाल लेते हैं।
भारत में पुलिस अपने आप में एक सामाजिक इकाई भी है। वह एक बड़ा सोशल पावर स्ट्रक्चर है। भारतीय समाज में पुलिस पावर की प्रतीक है, यूरोप की तरह सेवा की नहीं। पावर भारतीय समाज का एक बड़ा मूल्य है। चूंकि हमारे समाज का लोकतांत्रिकीकरण ठीक से नहीं हो सका है इसलिए यहां ताकत को काफी प्रतिष्ठा प्राप्त है।
पुलिस में जाना एक तरह से ताकत प्राप्त करना और उसका इस्तेमाल करना है। वर्दी वर्चस्व की प्रतीक है। एक साधारण सिपाही भी कमजोर तबकों पर रौब जमाना अपनी शान समझता है।
ताकतवर के साथ पुलिस
समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मकता, वर्णवाद, हिंदूवाद और सामंती मानसिकता पुलिस के चरित्र को एक खास रूप देती है। किसी थाने में बलात्कार की शिकार महिला के साथ जो बदतमीजी की जाती है, क्या वह राजनीतिक दबाव की देन है? आखिर क्यों एक गरीब आदमी की फरियाद नहीं सुनी जाती? निचली जाति के व्यक्ति को अपमानित करने के पीछे कौन सा राजनीतिक निर्देश काम करता है? आखिर क्यों मालिक-मजदूर की लड़ाई में पुलिस स्वाभाविक रूप से मालिकों के पक्ष में खड़ी हो जाती है?
अल्पसंख्यकों के प्रति पुलिस की कठोरता को समाज से समर्थन मिलता है। दंगों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुलिसिया कार्रवाई पर हिंदू समाज चुप ही नहीं रहता बल्कि उसका समर्थन करता है। अल्पसंख्यक विरोधी पुलिसवाले अक्सर हीरो बना दिए जाते हैं।
यह कैसी विडंबना है कि एक समुदाय पर कहर ढाने वाला दूसरे समुदाय का नायक बन जाता है।
मीडिया की भूमिका
अक्सर पुलिस में जातीय गौरव देखा जाता है। फिल्मों में देखिए। किस तरह एनकाउंटर या अपराधी को पुलिस द्वारा खुद ही सजा दिए जाने का महिमामंडन किया जाता है। मीडिया का एक हिस्सा भी इसमें लगा रहता है। अभी कुछ समय पहले हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठे तो अच्छे-खासे पढ़े लिखे लोगों ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। यहां तक कि जनांदोलनों पर पुलिस दमन का मध्यवर्ग समर्थन करता है।
पिछले दिनों मैंने कई संभ्रांत घरों के लोगों और यहां तक कि महिलाओं को जामिया मिलिया में छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते सुना। इन लोगों का कहना था कि जेएनयू जैसे संस्थान को बंद कर देना चाहिए। जाहिर है, पुलिस को अपनी हिंसा के लिए ताकत समाज से ही मिलती है।
जहां तक स्वायत्तता देने का प्रश्न है, तो अतीत में कुछ उत्साही मुख्यमंत्रियों ने पुलिस को ‘फ्री हैंड’ देकर वाहवाही लूटने की कोशिश की है। उस दौर में पुलिस की ज्यादती का शिकार सबसे ज्यादा सरकार विरोधी आंदोलनकारी हुए। लेकिन जब कुछ ताकतवर समुदाय आरक्षण जैसी मांग को लेकर सामने आते हैं तो पुलिस के हाथ-पांव फूल जाते हैं।
दोषी अफ़सरों पर हो कार्रवाई
इसलिए छोटे-मोटे सुधारों से बात नहीं बनेगी। पुलिस बल की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। पुलिस की अनुचित हरकतों का विरोध करना होगा। अनियमितता के दोषी अधिकारियों को हर हाल में दंडित करने के लिए दबाव बनाना होगा। अपने अन्य बुनियादी अधिकारों की मांग के साथ एक संवेदनशील, विवेकशील और जिम्मेदार पुलिस बल की भी मांग करनी होगी। जाहिर है, यह एक बेहतर समाज और व्यवस्था बनाने के संघर्ष का ही हिस्सा होगा।

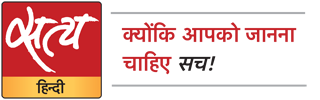




























अपनी राय बतायें