“हर अमृता को रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस चाहिए, थप्पड़ वाला प्यार नहीं”
ऐसी उम्मीद दिवास्वप्न है।
कहाँ है? किस व्यवस्था से उसे उम्मीद है? वर्तमान पारिवारिक ढाँचे में तीन हज़ार साल से कोई बदलाव नहीं आया तो अब क्या आएगा? नसों में जो ग़ुलामी उतार दी गई है, उसे कैसे बाहर निकालेंगे? थप्पड़ एक फ़िल्म नहीं, स्त्री के स्वाभिमान का लहूलुहान चेहरा है। सदियों के थप्पड़ों का दाग चाँद पर है और स्त्री का चेहरा वही चाँद है। आप चाँद के चेहरे पर दाग़ के अर्थ ढूँढना बंद कर दीजिए। उसका जवाब आपकी ऊंगलियाँ हैं जो सदियों से किसी स्त्री का गाल ढूँढती चली आई हैं। चाँद के चेहरे पर झाइयाँ नहीं है वो दाग़। आपके ज़ुल्मों सितम की कहानी है... हिंसा की लिपि पुरुषों से बेहतर कौन लिख और पढ़ सकता है? हिंसा की लिपि कई स्तरों पर लिखी जाती है। मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर।
स्त्री के गाल और उसकी देह तो पहले से ही उस लिपि के लिए स्लेट का काम करते थे, अब उसकी आत्मा पर थप्पड़ के फफोले उगने लगे हैं।
सवाल एक थप्पड़ का नहीं है बाबा। मत ढूँढिए। न ही तर्क दीजिए कि एक ही थप्पड़ तो मारा था। इतना तो चलता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। औरत को सहने की आदत डाल लेनी चाहिए।
याद दिलाऊँ।
तीन हज़ार साल पहले भिक्षुणी सुमंगला ने आज की अमृता की तरह ही थप्पड़ खाकर लिखा था कि “अहो, मैं मुक्त हुई। मेरा पति तो मुझे उस छाते से भी तुच्छ समझता था जिसे अपनी जीविका के लिए बनाता था।”
अमृता (तापसी पन्नू) का पति उसे क्या समझता रहा? फ़िल्म देखने वाले दर्शकों से क्या छुपा है? उनकी आत्मा जानती है कि लोग अपनी पत्नियों को क्या समझते हैं?
एक गाल जिस पर दुनिया भर का ग़ुस्सा और कुंठा छाप दिया जा सकता है। एक सामान जिसे जब चाहे अपने घर से निकलने का हुकुम दिया जा सकता है।
एक देह जिसे जब चाहे बिस्तर पर पटका जा सकता है, रौंदा जा सकता है। उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध।
एक वर्कर जिसे जब चाहे घरेलू कामों में झोंका जा सकता है। रसोई जिसकी सबसे बड़ी जगह। जहाँ उसे हर हाल में आग में पकना, सींझना है।
एक कोख, जिसे संतानोत्पति के लिए जब चाहे लोड किया जा सकता है। वंश वृद्धि के नाम पर संतानें पैदा करते रहने का हुक्म दिया जा सकता है।
एक भ्रूण, मांस का लोथड़ा जिसका पता लगते ही कोख में ही कत्ल किया जा सकता है। ये तो कम है। जाने कितनी बातें गिनाई जा सकती हैं।
इन सबके वाबजूद थप्पड़ तो इनाम है, रोज़ की बात है, उसका चाय और नाश्ता है। कहते हैं– घर तो स्त्री से बनता है। मकान को घर वही बनाती है। कितना कड़वा सच है कि वह घर ही तो उसकी कब्रगाह है। वो घर कहाँ होता है उसका। संपत्ति में कहाँ होता है उसका नाम। पति को ग़ुस्सा आए तो बाल पकड़ कर दरवाज़े से बाहर धकिया सकता है। उसका सामान बाहर फेंकते हुए चुटकी बजाते हुए कह सकता है… निकलो बाहर, अभी के अभी निकलो… ये घर मेरा है...।
एक चुटकी सिंदूर की क़ीमत एक चुटकी है। जो उसे पल भर में दर-बदर कर देती है। आधी रात को अपना सामान लेकर कहाँ जाए। बेशर्म औरतें फिर भी वहाँ पड़ी रहती हैं। नयी पीढ़ी की अमृता बेशर्म स्त्री नहीं है। उसमें स्वाभिमान बाक़ी है। वह उस रिश्ते में, उस घर में रहने से इंकार कर देती है।
फ़िल्म में एक जगह वह कहती है, "पता है उस थप्पड़ से क्या हुआ? उस एक थप्पड़ से ना मुझे वो सारी अनफ़ेयर चीजें साफ़-साफ़ दिखने लग गईं जिसको मैं अनदेखा करके मूवऑन करती जा रही थी।"
अमृता अब तक अपनी शादी में अपनी जगह ढूंढ रही थी। उसे चोट लगी। क्योंकि उसने अपने लिए अलग से थोड़ी-सी ख़ुशी भी नहीं बचा रखी थी। इस रिश्ते से बाहर आकर अब उसे अपने खालीपन को भरना है। वह बहुत साफ़-साफ़ कहती है, "उसने मुझे मारा; पहली बार। नहीं मार सकता। बस इतनी सी बात है। और मेरी पिटिशन भी इतनी-सी है।"
बस इतनी-सी बात समाज को और मामूली लगती है। बस अमृता की लड़ाई इस थप्पड़ को मामूली नहीं बनने देने की है। थप्पड़ तो एक बहाना है, उसके माध्यम से समाज के सारे सगे-संबंधियों के असली चेहरे, उनकी भूमिका एक्सपोज हो जाती है।
थप्पड़ का असर
थप्पड़ अमृता (तापसी पन्नू) को लगता है मगर उसका असर उसकी पड़ोसी शिवानी (दिया मिर्ज़ा), उसकी माँ संध्या (रत्ना पाठक शाह), उसकी सास सुलक्षणा (तन्वी आज़मी), उसकी वकील नेत्रा (माया), उसकी हाउस हेल्पर (गीतिका विद्या) के जीवन में भी पड़ता है। सबके दुख उजागर होते हैं। अपने अरमानों के कब्रगाह पर बैठी मातमी ये सभी स्त्रियाँ शोक-पत्र की तरह पढ़ी जा सकती हैं।
ये स्त्रियाँ ऊपर-ऊपर शांत जीवन जी रही हैं। उनके भीतर जीवन जैसे थम चुका है। इसीलिए उन्हें एक थप्पड़ पर आश्चर्य नहीं होता। न ही कोई अफसोस। ये तो होता रहता है… टाइप मसला है। रात को लात-जूते खाओ, सुबह काम पर जाओ। भूल जाओ...आगे बढ़ो।
मेरे गाल, तुम्हारे थप्पड़… जश्न मनाओ।
सास कहती है- औरतों को बर्दाश्त करना सीखना चाहिए।
माँ कहती है- मैंने नहीं सहा, बहुत कुछ करना चाहती थी, परिवार के लिए सब छोड़ दिया।
पति कहता है- मैं ग़ुस्से में था, तुम बीच में आ गई।
भाई कहता है- उस वक़्त वो तनाव में था, हो गया। हमें समझना चाहिए।
सबके पास अपने जस्टिफ़िकेशन हैं, तर्क हैं। किसी के पास एक सॉरी नहीं है। किसी को नहीं लगता कि ये ग़लत हुआ, बहुत ग़लत।
फ़िल्मकार अनुभव सिन्हा यहाँ सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मुल्क और आर्टिकल-15 जैसी फ़िल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा का यह थप्पड़ हिंदी सिनेमा को याद रहेगा।
लेकिन इस फ़िल्म को घरेलू हिंसा के खाँचे में न डालें। घरेलू हिंसा का सतही अर्थ निकालते हैं हम। यातना का कोई पैटर्न सेट है क्या। रात-दिन ताने मार कर मुर्दा कर देना, किस खाँचे में डालेंगे। आपकी कसौटी पर खरी न उतरने वाली, औरत की आत्मा को छीलते जाने को क्या कहेंगे। भोजन-प्रेमी पेटुओं की पत्नियों को छप्पन भोग बनाना आना चाहिए, नहीं तो वे घरेलू सहायिकाओं को गले लगा लेंगे। जो उनकी लपलपाती जिह्वा के लिए भोजन तैयार करती रहती है। मध्यवर्गीय पुरुषों को अपनी औरतें काम पर दिखनी चाहिए। चाहे बच्चा उठाए हों या रसोई में खटर-पटर करती हुई। एक भुक्तभोगी औरत ने कहा था- “आप कोई काम मत करो, जब पति घर में हों, तो बस उसके सामने काम करती हुई दिखो… उन्हें यह बात बहुत भाती है कि उनकी बीवी कितना काम करती है, उनके लिए कितनी समर्पित है।”
पाखंड करो… प्रेम का पाखंड, समर्पण का पाखंड... ऐ जी, वो जी करते रहो, आरती उतारते रहो, नहीं तो वो आत्मा छील कर सुखा देंगे।
अनुभव सिन्हा यहाँ उनको एक्सपोज कर देते हैं। सिनेमाई खाँचे तोड़ देते हैं। इसीलिए इस फ़िल्म को किसी जॉनर में न रखें। फ़िल्म थ्योरिस्ट रॉबर्ट स्टेम का मानना है कि कुछ बेहतरीन फ़िल्मों को जॉनर फ्री रखना चाहिए।
सारे पात्र एक-दूसरे से जुड़े
अनुभव की यह फ़िल्म वैसी ही है। सबसे अलग, सबसे जुदा। अलग शैली में अपनी कथा कहती हुई। फ़िल्म को प्रारंभ से ही ध्यान से देखना चाहिए। कथा-कोलाज से कुछ दृश्य है, अलग-अलग फ्रेम में। अलग-अलग पात्र हैं, उनकी बातें हैं, उनके सुख-दुख हैं। बाद में सारे पात्र एक-दूसरे से जुड़ते हैं। सबके जीवन में कोई न कोई समस्या चल रही है। सबके केंद्र में स्त्री है। यह स्त्री सिनेमा है या स्त्री के बहाने ज़िंदगी का सिनेमा है। ज़िंदगी अपने आप में एक जॉनर है। निर्मम और संघर्षपूर्ण। उसके पास दया-माया नहीं।
औरत तो दोहरा शिकार है। एक तो ज़िंदगी का कहर, ऊपर से उसकी ज़िंदगी भी अपने नियंत्रण में नहीं। विवाह उसके लिए “होलोकास्ट” साबित होता है। जिसमें अपना मन, इच्छाएँ और स्वप्न सब किसी और के नियंत्रण में दे देना होता है। विवाह एक यातना शिविर बन जाता है उसके लिए।
यह फ़िल्म उसी यातना शिविर से बाहर निकलने का शंखनाद है। एक सलाह भी है कि वैवाहिक हिंसा को रोकना हो तो पहले थप्पड़ पर ही प्रतिवाद ज़रूरी है। हिंसा के बदले हिंसा की पैरोकारी नहीं करती यह फ़िल्म। फ़िल्म की नायिका अमृता चाहती तो भरी पार्टी में पति के थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे कर हिसाब बराबर कर सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि प्रतिशोध लेना उसका मक़सद नहीं था। अपने कंफ़र्ट ज़ोन से बाहर निकल कर दुनिया को मैसेज देना ज़रूरी था।
बस एक क़दम, एक क़दम की दूरी पर है रिहाई।
नायिका बिल्कुल लाउड नहीं होती है। कोई चीख या चिल्लाहट या विलाप उसके एक्शन में नहीं है। उसके पास है तो सिर्फ़ थोड़ी-सी ख़ुशी पाने की चाहत। उम्मीदें जो अब भी कहीं बची हुई थीं। अंधेरे में जुगनू भी रोशनी की उम्मीद की तरह होता है।
उम्मीद की चिंगारी
अनुभव की एक बात माननी पड़ेगी...
वे अपने पात्रों के प्रति बहुत क्रूर नहीं होते। फ़िल्म को दुखांत और सुखांत के बीच झूला बना कर छोड़ देते हैं। या कहें कि एक उम्मीद की चिंगारी छोड़ देते हैं। वे मानते हैं कि किसी इंसान में सुधार की गुँज़ाइश हमेशा होती है। अंत बिल्कुल फ़ॉर्मूलाबद्ध नहीं कि तलाक़ के पेपर पर साइन होने से पहले दोनों मिल जाएँ। स्त्री का दिल पिघल जाए, वह माफ़ कर दे। दर्शक ख़ुश, पैसा वसूल। यह मक़सद नहीं था अनुभव का। मगर उन्होंने नायक के मुँह से सॉरी बुलवाया और यह कहलवाया कि वह अमृता का दिल फिर से जीतने की कोशिश करेगा।
पता नहीं, वह कितना कामयाब हुआ, या नहीं हुआ… बीच में एक बच्चा भी है, जो अमृता के गर्भ में है। उसके आने के बाद क्या परिस्थितियाँ रहेंगी, यह सब कुछ दर्शकों के सोचने के लिए छोड़ दिया।
अनुभव ने फ़िल्म में कुछ पात्रों को बहुत सपोर्टिव दिखाया है। सारे पति हिंसक नहीं होते। जैसे दिया मिर्ज़ा के दिवंगत पति। सपोर्टिव पुरुष जैसे नायिका का पिता। जैसा आजकल के पिता होते हैं। वे पत्नियों के मामले में बेहद संकीर्ण होते हैं, बेटियों के मामले में उनका व्यवहार उल्टा होता है। वे बेटियों के साथ हर लड़ाई में डट कर खड़े होते हैं। अपना दरवाज़ा उसके लिए खुला रखते हैं। यहाँ माँ का किरदार कटघरे में है जो यह मानती है कि बेटी का असली घर उसका पति का घर होता है। बहुत बड़ा छलावा है, फरेब है औरतों के साथ। औरतों को बताइए कि तेरा कोई घर नहीं होता बन्नो। अपने दम बना घर।
अमृता की वकील है, नेत्रा (माया) उसका किरदार एकदम रियल है। धनाढ्य पति और ससुर के दम पर वकालत में अपना सिक्का जमाती है, मगर उसका दम घुटता है। क्योंकि वह पति की नज़र में सिर्फ़ एक सेक्स ऑब्जेक्ट है। एक ऐसी स्त्री जो उसकी पोजीशन का लाभ लेकर सफलता हासिल करती है। अंत में उस धन दौलत, पोजीशन सबको ठोकर मार कर ख़ुद को पिंजरे से आज़ाद कर लेती है।
एक कामवाली बाई है। रोज घर में पति पीटता है। अंत में वह हाथ उठा लेती है। पति को पीटती हुई कहती है- “तू पीट मुझे, मगर मुझे ज़िंदगी तो जी लेने दे..।“
एक स्त्री है, दिया मिर्ज़ा । सिंगल मदर, विधवा है। उसकी किशोर बेटी उसके लिए साथी ढूंढना चाहती है। नहीं मिलता तो अंत में माँ, बेटी दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अकेले ही वे ज़्यादा ख़ुश हैं।
सिंगल औरतें हर थप्पड़, हर धौंस और हर क़ैद से मुक्त हैं। मन का साथी न मिले तो एकल जीवन सबसे बेहतर विकल्प।

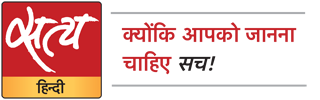

































अपनी राय बतायें