बीता साल पंजाबी साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर अमृता प्रीतम का जन्मशती वर्ष था। जन्मशती वर्ष पर जिस तरह से अमृता को याद किया जाना और उनके साहित्य पर बात होनी चाहिए थी, वह पूरे देश में कहीं नहीं दिखाई दी। सरकारों और उसके पैसे से चलने वाली तमाम साहित्यिक अकादमियों को तो छोड़ ही दीजिए, जिस पंजाबी भाषा की वह लेखिका थीं, उसके बोलने—पढ़ने वालों ने भी उन्हें बिसरा दिया। जबकि इस ज़बान को बरतने वाले, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं।
31 अगस्त, 1919 में अविभाजित भारत के गुजरांवाला में जन्मी अमृता प्रीतम, पंजाबी ज़बान की पहली कवयित्री मानी जाती हैं। भारत-पाक बँटवारे पर लिखी, उनकी लंबी नज़्म ‘आज आखां वारिस शाह नु तू कब्रा विच्चों बोल’ भारत और पाकिस्तान दोनों जगह काफ़ी मक़बूल हुई। सौ से ज़्यादा किताबें लिखने वालीं अमृता प्रीतम ने साहित्य की हर विधा में काम किया। मसलन; कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, पंजाबी लोक गीत और आत्मकथा।
उर्दू अदब की नामचीन लेखिकाओं इस्मत चुग़ताई, कुर्तुल-एन-हैदर की लेखन परंपरा से क़दम ताल मिलाने वाली पंजाबी-हिन्दी भाषा की अनन्य लेखिका अमृता प्रीतम को हालाँकि, मुसलिम समाज की तरह अपनी रिवायतों में बंधे मुसलिम समाज की बनिस्बत खुला समाज मिला, मगर औरत की ज़िंदगी को उन्होंने हर जगह, हर कौम में एक सा पाया। दुनियावी बदलाव-अतिक्रमणों से दूर औरत की ज़िंदगी का भूगोल अभी तक अक्षुण्ण है। क्योंकि उसे आज भी अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने और फ़ैसले लेने का अधिकार नहीं है। औरत की ज़िंदगी की अंदर और बाहर की यही कशमकश हमें अमृता प्रीतम के कमोबेश सभी उपन्यासों और कहानियों में दिखलाई देती है।
हालिया वक़्त में हिन्दी साहित्य में नारी विमर्श के नाम पर जिस तरह नारीवादी लेखक-लेखिकाओं ने औरत की वास्तविक समस्याओं से इतर जो थोकबंद लिखा-रचा है, वह हमारे अन्दर की यौन जुगुप्सा को तो जगाता है, लेकिन हमें उनके हक में खड़ा नहीं करता। इसके विपरीत अमृता प्रीतम के सभी उपन्यास औरत को समाज में मान-सम्मान लौटाए जाने के आख्यान हैं। ‘एक थी सारा’, ‘कच्ची सड़क’, ‘उन्नचास दिन’, ‘पिंजर’ आदि अपने सभी उपन्यासों में उन्होंने औरत को बिल्कुल अलहदा ढंग से ही बयाँ किया और उसे अपनी आवाज़ दी। औरत की आर्थिक, सामाजिक आज़ादी की हिमायती अमृता प्रीतम अपनी आत्मकथा ‘रसीदी टिकिट’ में खुलकर अपने अंतःकरण की बात करती हैं। अपनी मोहब्बत और चाहत, शायर-गीतकार साहिर लुधियानवी से अपने प्यार भरे संबंधों को कबूलती हैं। यही नहीं, चित्रकार इमरोज से उनके जो आत्मीय रिश्ते थे, उसे भी नहीं छिपातीं। उस ज़माने में जब हिंदुस्तानी समाज इतना खुला समाज नहीं था, तब इतनी बेबाकी से यह सब लिखना, वाक़ई अमृता प्रीतम के ही बूते की बात थी।
अमृता प्रीतम ने देश का बँटवारा देखा था। बँटवारे के बाद वह दिल्ली आ गई थीं। यही वजह है कि मुल्क की अवाम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बाँट देने वाले बँटवारे का दर्द उनके अदब में साफ़ दिखलाई देता है। ख़ास तौर पर उपन्यास ‘पिंजर’ में।
यूँ तो भारत-पाक बँटवारे पर यशपाल का ‘झूठा सच’, भीष्म साहनी का ‘तमस’, डॉ. राही मासूम रजा का ‘आधा गाँव’, बलवंत सिंह का ‘काले कोस’, अब्दुल्लाह हुसैन का ‘उदास नस्लें’ आदि विचारोत्तेजक उपन्यास लिखे गये हैं, जो हमारे बीते हुए माज़ी के ऐतिहासिक दस्तावेज़ हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण उपन्यासों के बीच अमृता प्रीतम ने अपने उपन्यास ‘पिंजर’ में विभाजन की पीड़ा के दरमियान स्त्री सवालों को जिस तेवर से उठाया है, वह ‘पिंजर’ को बाक़ी उपन्यासों से अलग बनाता है।
इन सवालों की पड़ताल, हमें ऊपर ज़िक्र किए गए उपन्यासों में भी देखने को मिलती है लेकिन औरत के दुख-दर्द, संघर्ष, विषाद, वेदना की जो तसवीरें अमृता प्रीतम ने ‘पिंजर’ में बनाई हैं, वे उस भीषण दौर की हक़ीक़त के ज़्यादा नज़दीक हैं।
‘‘दिन के प्रकाश में पूरो हमीदा बन जाती थी। रात के अंधकार में वह पूरो रहती, किन्तु पूरो सोचती थी वह वास्तव में हमीदा थी न पूरो, वह केवल एक पिंजर थी। केवल पिंजर, जिसका कोई रूप न था कोई नाम न था।’’
उपन्यास ‘पिंजर’ की यह वैचारिक शुरुआत, एक मुकम्मल कहानी बयाँ कर जाती है। पूरो और हमीदा के नाम के बीच झूलती औरत की ख़ुद को तलाशने-पहचानने की कहानी है, अमृता प्रीतम का उपन्यास ‘पिंजर’।
उपन्यास ‘पिंजर’ का कथानक साल 1935 से शुरू हो, साल 1947 भारत-पाक विभाजन के काल तक फैला हुआ है। मौजूदा दौर में हिन्दू-मुसलिम रिश्तों में तनाव की जो प्रक्रिया बनी है, वह आकस्मिक नहीं है बल्कि यह वैमनस्य, संघर्ष आपस में छोटे-छोटे फिरकों के बीच अपने क्षुद्र हितों के चलते बराबर चलता रहता था। जिसका सीधा-सीधा तआल्लुक आर्थिक कारणों से था न कि धार्मिक।
विभाजन की तटस्थ विवेचना
कालांतर में हमारे हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के दो बड़े सम्प्रदायों को किस तरह वास्तविक समस्याओं से काट काल्पनिक समस्याओं, आपसी डर, चिंताओं से बाँध दिया, यह विवेचना का बिंदु हो सकता है। विभाजन की तटस्थ विवेचना के बाद ही धार्मिक, भाषायी आधार पर बँटवारे का मिथक टूट सकता है। सच बात तो यह है कि उपन्यास ‘झूठा-सच’, ‘आधा गाँव’, ‘तमस’, ‘पिंजर’ के ज़रिए ही हम बँटवारे से पहले हिंदुस्तानी समाज में घट रही उन घटनाओं से वाकिफ हो सकते हैं, जिनका कि किसी इतिहास में ज़िक्र नहीं मिलता। भारत-पाक बँटवारे का जो दिग्भ्रमित कोहरा नई पीढ़ी के ज़हन में अंकित है, वह कोहरा बहुत हद तक इन उपन्यासों के पढ़ने से छँट सकता है।
जहाँ यशपाल, भीष्म साहनी अपने उपन्यासों में भारत-पाक बँटवारे से जुड़े राजनीतिक सवालों की गहन जाँच-पड़ताल करते हैं, वहीं अमृता प्रीतम सामाजिक, आर्थिक वजह की नुक्ता-ए-नज़र में बँटवारा देखती हैं। उनकी नज़र में बँटवारा ऐसी मानवीय त्रासदी थी, जिसमें कि औरत को ही सबसे ज़्यादा नुक़सान हुआ।
पिंजर की कहानी
यह महज़ इत्तिफ़ाक़ ही है कि इस सदी के दूसरे भयानक दंगे देखने वाली गुजरात की सरज़मीं से ही ‘पिंजर’ की कहानी शुरू होती है। कहानी मुख्तसर सी है, गुजरात के एक छोटे से गाँव छत्तोआनी में रहने वाले शेखों और शाहों के बीच आपसी टकराव चलता रहता था। जिसका पलड़ा भारी होता, वह दूसरे पर हावी हो जाता। शेखों और शाहों के बीच यह तनाव आर्थिक वजह से ज़्यादा था। गाँव में सामंतवाद-जातिवाद का बोलबाला था।
भारतीय समाज में यह वाक्य मशहूर है कि ‘औरत ही औरत का दु:ख समझ सकती है।’ लेकिन इसके उलट एक सच्चाई यह भी है कि ‘औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है।‘ पूरो की माँ उससे कहती है, ‘‘हम तुझे कहाँ रखेंगे?, तुझे कौन ब्याह कर ले जाएगा?, तेरा धर्म गया तेरा जनम गया।’’ नौ माह अपने गर्भ के अंदर रखने वाली माँ, जब अपनी बेटी के दु:ख-दर्द उसकी मानसिक स्थिति नहीं समझ पाती, तो पूरो की आख़िरी उम्मीद भी टूट जाती है। पूरो, रशीद के घर वापिस लौट आती है और यहीं से उपन्यास ‘पिंजर’ का असली कथानक शुरू होता है।
‘पिंजर’ सिर्फ़ पूरो की ही कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी नवविवाहिता तारो, पूरो की भाभी लाजो, बारह बरस की लड़की कम्मो और पगली की भी आपबीती है। अमृता प्रीतम ने पूरो के साथ-साथ इन किरदारों के मार्फत उस ज़माने में स्त्री समस्या से जुड़े हुए उन सवालों को भी खोजने की कोशिश की है, जिनके जवाब आज भी बमुश्किल से मिलते हैं। सदियों से समाज में उपेक्षित, प्रताड़ित, शोषित नारी की दशा पर उनका चिंतन सार्वकालिक दिखता है। उपन्यास के महिला पात्रों के ज़रिए अमृता प्रीतम ने जो संवाद और जुमले कहलवाए हैं, वे काबिले ग़ौर हैं। मसलन,
‘‘तारो-लड़कियों का क्या है? माँ-बाप चाहे जिसके हाथ में उसके गले की रस्सी पकड़ा दें।’’
‘‘वहां का पानी अच्छा है? पूरो ने पूछा
‘‘अच्छा नहीं हो तो भी अच्छा ही है। दूसरों के दुःख की कौन परवाह करता है? बल्कि फिर वह लोग कहते हैं, हम रोटी देते हैं। कपड़ा देते हैं। खुला हाथ है, फिर किस बात का दुःख है?”
‘‘जैसे औरत को केवल रोटी और कपड़ा ही चाहिए।’’ पूरो ने कहा।
‘‘मेरे हृदय में आग सी धधक उठती है। तू नहीं देखती, सब देखते हैं। पूरे दो बरस हो गये हैं, रोटी और कपड़े के लिए उसे अपना शरीर बेचती हूँ। देख मैं वैश्या हूँ......मैं वैश्या हूँ।’’
कहते-कहते तारो गिर पड़ी।
‘‘पूरो सोचती रही, सब गीत सुंदर लड़कियों के ही गुण गाते हैं। सारे भजन सच्चे प्रेम का ही वर्णन करते हैं। क्या कभी ऐसे गीत भी बनेंगे, जिसमें मुझ जैसी लड़कियों के रूंदन की कथा लिखी जाएगी? क्या कभी ऐसे भजन भी होंगे, जिनका कोई भगवान नहीं होगा?’’
चुनांचे, उपन्यास में पूरो की यही चिंतन यात्रा औरत के अपने होने, न होने का दुःख तंत्र है। क्या वह सिर्फ़ एक जरखरीद ग़ुलाम है? या आदमी द्वारा हथियाया हुआ आख़िरी उपनिवेश! आदमी की निरंकुश सत्ता से उसका ख़ुद का वजूद कहीं खो सा गया है।
औरत की ज़िंदगानी से जुड़े हुए इन सवालों से जूझते हुए, अमृता प्रीतम ने बँटवारे का जो मंजर खींचा है, वह काफ़ी दर्दनाक है।
दंगों की हैवानियत में औरतों के साथ जो बर्ताव, जोर-जुल्म होता है, उस जुल्मों-सितम की बानगी हमें उपन्यास के इस दृश्य में दिखती है-
“पूरो के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते पर उनका कोई उत्तर नहीं मिलता। उसे पता नहीं चलता था कि अब इस धरती पर जो कि मनुष्य के लहू से लथपथ हो गई थी, पहले की भाँति गेहूँ की सुनहरी बालियाँ उत्पन्न होंगी या नहीं। इस धरती पर जिसके खेतों में मुर्दे पड़े सड़ रहे हैं, अब भी पहले की भाँति मकई के भुट्टों में से सुगंध निकलेगी या नहीं। क्या ये स्त्रियाँ, इन पुरुषों के लिए अब भी संतान उत्पन्न करेंगी, जिन पुरुषों ने स्त्रियों के साथ ऐसा अत्याचार किया था।’’
उपन्यास में पूरो के मन का यह रूंदन, बँटवारे के बाद हुए दंगों की विभीषिका उजागर करता है। भारत-पाक बँटवारे के बाद पूरो की भाभी बँटवारे में पाकिस्तान की सीमा में चले गए, अपने ही घर में कैद कर ली जाती है। रशीद, पूरो की भाभी लाजो को बचाकर लाता है और सीमाओं के आर-पार हो रहे, लड़कियों के आदान-प्रदान में लाजो को उसके घर वालों के सुपुर्द कर देता है। इस तरह रशीद की रूह पर सालों से पड़ा भारी बोझ सरकता चला जाता है। यहीं पूरो का दिल एक बारगी सोचता है कि गर वह भी कह दे कि वो एक हिन्दू स्त्री है, तो उसके घर वाले उसे अपने साथ ले जाएँगे। हज़ारों लड़कियों की तरह वह भी अपने घर जा सकती है, लेकिन पूरो मना कर देती है। पूरो का मंगेतर रामचंद्र जिसने पूरो को उस समय जब वह रसीद के घर से भागकर उसके पास आ गई थी, अपनाने से इनकार कर दिया था, अपनी करनी के लिये माफ़ी माँगता है और उपन्यास के अंत में पूरो से हाथ जोड़कर विदा लेता है।
बहरहाल, अमृता प्रीतम ने जिस तरह उपन्यास का अंत किया है, उसमें उस दौर के लिखे गए साहित्य की तरह ही मोहक आदर्शवाद की झलक दिखती है। इस सबके बावजूद भारतीय संदर्भ में स्त्री विमर्श के संपर्क सूत्र तलाशें तो उन्नीसवीं सदी में लिखी गयी ताराबाई शिंदे की किताब ‘स्त्री पुरुष की तुलना’ के बहुत बाद, अमृता प्रीतम के उपन्यास ‘पिंजर’ में यह स्त्री विमर्श प्रमुखता से दृष्टिगोचर होता है। यही वजह है कि अमृता प्रीतम और उनका साहित्य दोनों ही आज भी हमारे लिए बेहद अहम और ज़रूरी है। उनके साहित्य की प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं होगी।

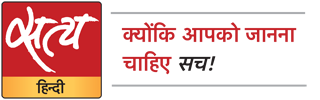




























अपनी राय बतायें