दो-ढाई हफ़्ते से मेरा लिखना-पढ़ना बंद-सा था। अपने यू-ट्यूब कार्यक्रमों से भी दूर था। बाहरी बंदिश न होने के बावजूद कुछ लिख-पढ़ या सार्वजनिक तौर पर बोल न पाने की अशक्तता या मजबूरी कितनी भयानक होती है, लगातार इसे शिद्दत के साथ महसूस किया। पर अब धीरे-धीरे अपने काम-काजी जीवन में वापसी हो रही है।
इस दरम्यान देश-दुनिया और अपने आसपास काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन चाहते हुए भी लिखना या बोलना संभव नहीं था। सिर्फ़ सोचता रहा। आदमी भी अद्भुत जीव है, किसी मजबूरी में वह चाहे जितना निष्क्रिय या शिथिल हो पर सोचना बंद नहीं करता। ज़िंदगी जब तक साथ रहती है, वह सोचता रहता है।
बीते दिनों की कुछ बड़ी घटनाओं में कुछेक पर लिखने का इरादा है। पर कौन जाने, आगे क्या-क्या होगा और कितना अच्छा या कितना भयावह होगा, जिससे बीते दिनों के तमाम घटनाक्रम पीछे छूट जाएँ। इसलिए एक-एक घटनाक्रम पर सिलसिलेवार लिखने के बजाय मैं इस बार अपने कॉलम में सिर्फ़ कुछ ‘आब्जर्वेशन’ दर्ज कर रहा हूँ।
देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के साथ एक शब्द उछला था- विनिवेश। पूर्ण या आंशिक निजीकरण के लिए सुंदर-सा नाम! कांग्रेसी शासन में शुरुआत हुई लेकिन विनिवेश के नाम पर बाक़ायदा एक अलग केंद्रीय मंत्रालय खड़ा करने का दुस्साहस ‘जनसंघी-डीएनए’ वाले एनडीए-1 ने ही दिखाया। मज़े की बात है, इस सरकार में बीते जमाने के सबसे तेज़तर्रार समाजवादी जार्ज फर्नांडीज भी शामिल थे और काफ़ी प्रभावशाली हैसियत के साथ। एक जमाने में देश की राजनीति में सिर्फ़ दो संगठन- जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीमित कर उन्हें निजी क्षेत्र और उद्योगपतियों को सौंपने की खुली वकालत करते थे। लेकिन आर्थिक सुधार के दौर ने उस विमर्श को ही बदल डाला। जब अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए-1 की सरकार बनी तो बाक़ायदा विनिवेश मंत्रालय बन गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े उपक्रमों को निजी हाथों में औन-पौन दाम पर बेचा गया। कई विवाद भी उठे। पर सिलसिला बढ़ता रहा। मौजूदा सरकार ने अब उन क्षेत्रों को भी निजी हाथों में सौंपने का सिलसिला तेज़ किया है जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। रेलवे, बीएसएनएल-एमटीएनएल, एयर इंडिया से लेकर तमाम बड़े सार्वजनिक उपक्रमों पर निजी क्षेत्र के वर्चस्व की धमक तेज़ हो गई है। पश्चिम के कई विकसित पूँजीवादी देश आज तक जिन कुछ सेक्टर्स को सरकारी क्षेत्र में रखे हुए हैं, भारत में वैसे उपक्रमों को भी निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और हैरत की बात कि कोई संगठित शक्ति बोलने या विरोध के लिए आगे नहीं आ रही है। इस भयावह दौर को क्या कहेंगे?
दमन-उत्पीड़न और ग़ैर-क़ानूनी हथकंडों के इस्तेमाल के मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस शुरू से ही बेहद कुख्यात रही है। लोगों की स्मृति से पुलिस के बारे में कही जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला की वे मशहूर लाइनें कभी ग़ायब नहीं होतीं, जिसमें उन्होंने इस शासकीय संगठन को ‘अपराधियों का सबसे संगठित गिरोह’ कह दिया था। यह छठे दशक की बात है। कई आयोग बने और ढेर सारे फ़ैसले आए। पर हालात कितना बदले हैं? अगर यूपी की स्थिति देखें तो मायूसी होती है: क्या सचमुच ऐसे तंत्र में लोक सुरक्षित है?
हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ रहे हैं।
मुठभेड़ हत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट तक चेता चुका है। मानवाधिकार आयोग में मामले दर्ज हैं और कई-कई बार नोटिसें जारी हुई हैं। पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पुलिस दमन, उत्पीड़न और लूटमार के अपने इतिहास में हर रोज़ नये पन्ने जोड़ रही है!
अचरज कि झाँसी के पुष्पेन्द्र यादव और बदायूँ के बृजपाल मौर्य की 'पुलिसिया हत्या' पर देश की सर्वोच्च सत्ता, मुख्यधारा मीडिया, न्याय विधान और मानवाधिकार के संवैधानिक संस्थान इस दौरान लगभग खामोश रहे। लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने सत्ता की निरंकुशता के साथ ही लोकतंत्र की इन संस्थाओं की खामोशी पर भी सवाल उठाए। पर क्या फ़र्क पड़ता है! सवाल उठाने वाले साधारण लोग थे।
बिहार में बारिश-बाढ़ की तबाही और सत्ता की आपराधिक निष्क्रियता, बंगाल में दिन-दहाड़े होती हत्याएँ, मुंबई में मेट्रो के पार्किंग शेड के लिए आरे की गज्झिन हरियाली और रातों-रात 2000 से ज़्यादा पेड़ों का सफ़ाया, कश्मीर में निरंकुशता का तांडव और एनआरसी के बहाने एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ संविधान विरोधी हथकंडों की बड़ी आज़माइश! और भी ढेर सारे मामले हैं!
ये तमाम उदाहरण यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि किसी देश में लोकतंत्र सिर्फ़ एक अच्छा संविधान पा जाने से या हर पाँच साल के अंतराल पर चुनाव कराने की औपचारिकता पूरी करने भर से नहीं स्थापित होता।
भीमा-कोरेगाँव का सच!
अभी आगे का देखिए! पता नहीं, क्या-क्या होने वाला है? पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा मामले में न्यायालय से फ़ैसला आना है। भीमा-कोरेगाँव में हिंसा किसी और ने की और कराई। पर एफ़आईआर के बावजूद उन तत्वों का बाल बाँका नहीं हुआ। शिव प्रतिष्ठान के विवादास्पद संभाजी भिड़े और अन्य लोगों पर लंबित मामलों को महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने वापस लेने का फ़ैसला किया। पर मशहूर अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज सहित आधे दर्जन लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता नवलखा को भी उसी मामले में लपेटने का जुगाड़ किया गया है। ‘सरकारी-जुगाड़’ सफल होता है या विफल, कोर्ट के फ़ैसले से तय होगा। उसी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। पर भीमा-कोरेगाँव का मामला चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुख्य विपक्षी गठबंधन कांग्रेस-एनसीपी के किसी मंच से उसका उल्लेख तक नहीं किया जा रहा है। हरियाणा हो या महाराष्ट्र-ये किस तरह के चुनाव हैं, जिसमें समाज और लोगों के वास्तविक मुद्दे नज़र तक नहीं आते! किसान, नौजवान, दलित, कामगार, महिलाओं और अन्य लोगों की मुश्किलों पर बात नहीं हो रही है।
सत्ताधारी नेता ताल ठोंक कर विपक्ष को हरियाणा और महाराष्ट्र में ललकार रहे हैं: ‘हिम्मत है तो बोलो, आर्टिकल 370 को संविधान में दोबारा शामिल करोगे?’ पर यह सवाल वे कश्मीर घाटी में नहीं उठा रहे हैं! वहाँ वे ‘विकास की बयार’ बहाने का आह्वान कर रहे हैं।
महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को कवर कर रहे कई पत्रकार-मित्रों से मैंने फ़ोन पर बातचीत की। इनमें कुछ दिल्ली से गए हैं और ज़्यादातर उक्त दोनों प्रदेशों में काम करते हैं। सबने एक स्वर में बताया कि इन प्रांतीय चुनावों के नतीजों में लोगों की उतनी दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही है। मामला चुनाव के सिर्फ़ सत्ता-प्रबंधन, मुद्रा-ज़ोर का नहीं है, ज़बर्दस्त मीडिया-मैनेजमेंट के ज़रिये समाज में पहले से ही एकतरफ़ा माहौल बनाया जा चुका है। विपक्ष दयनीय दिख रहा है क्योंकि उसके पास न तो कोई नय़ा एजेंडा है, न नया नेतृत्व है और न किसी तरह का सियासी जोश है। ईडी-सीबीआई से डर अलग से। कॉरपोरेट की तरफ़ से चंदा भी नहीं आ रहा है- सब एकतरफ़ा जा रहा है!
जेएनयू वाले का ‘झटका’
दिल्ली और यूपी सहित हिन्दी भाषी अन्य क्षेत्रों में एक बार फिर ‘अयोध्या’ पर गर्मी पैदा करने की कोशिश शुरू हो गई है। हिन्दी चैनलों का ज़्यादा ज़ोर अगले कुछ दिन इसी पर होगा। ज़ाहिर है, सर्वोच्च न्यायालय से फ़ैसला आना है। क्या 'न्यायिक फ़ैसला' होगा? कैसा होगा? उसके बाद क्या होगा? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं! इस बीच एक दिन की खलल पड़ी! बुरा हो रॉयल स्वीडिश एकेडमी वालों का, जिसने सोमवार को भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्तेय को अर्थशास्त्र में सन् 2019 के नोबल से सम्मानित करने का एलान कर दिया! अभिजीत ‘एंटी-नेशनल टुकड़े-टुकडे गैंग’ वाले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्नात्तकोत्तर हैं। वह आज भी जेएनयू के प्रशंसक हैं।
चिंताजनक स्थिति सिर्फ़ यह नहीं कि आज सत्ता इस कदर बेलगाम क्यों है, मीडिया इस तरह एकतरफ़ा क्यों है, न्यायतंत्र ऐसा निष्प्रभावी क्यों हो गया है। सबसे चिंताजनक स्थिति है कि आज हमारा समाज पूरी तरह विभाजित है।
उसका बड़ा हिस्सा अपने ही सामाजिक और राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम करने वालों के लिए तालियाँ बजा रहा है। ऐसे भटके हुए समाज को बटोरना, समझाना और फिर सुसंगत सामाजिक-राष्ट्रीय मुद्दों पर संगठित करना कोई आसान काम नहीं। सचमुच भारत को आज एक बड़े नेतृत्व, बड़े जन-संगठन और व्यापक नेटवर्क का शिद्दत से इंतज़ार है। पर आएगा कहां से? नये नेतृत्व या संगठन का उभरना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं होती, घटना-प्रतिघटना से जूझते समाज में एक ख़ास सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया में उभरते हैं नये नेतृत्व और नये संगठन। सिर्फ़ स्वतःस्फूर्तता ही नहीं, आत्मगत प्रयासों की भी ऐतिहासिक भूमिका होती है। अपने देश में ऐसे दो बड़े उदाहरण मौजूद हैं- महात्मा गाँधी और डॉ. भीमराव आम्बेडकर। दोनों दार्शनिक और विचार के स्तर पर काफ़ी अलग-अलग हैं पर दोनों ऐसे बड़े नेता हैं, जिन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास को बिल्कुल नये आयाम दिए। राष्ट्र के निर्माण की वैचारिक बुनियाद बनाई। एक की नृशंस हत्या की गई और दूसरे को सबने-मिलकर दरकिनार किया। पर आम्बेडकर और उनके विचारों की आज पूरे देश में धूम है। गाँधी आज भी राष्ट्रपिता हैं। पर दोनों का राष्ट्र आज सचमुच ख़तरे में है।

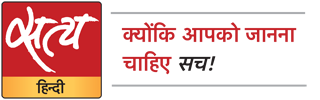





























अपनी राय बतायें