आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली में जीत के बाद भारत में नई किस्म की राजनीति पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इस बहस से 9 साल पहले की चर्चा की याद आ जाती है। तब 'आप' का उदय हुआ ही था। जातियों और धर्मों से परे जिसकी अपील हो, जो स्वच्छ राजनीति में यकीन करती हो, यानी जहाँ पैसे का लेन-देन नहीं है और जो पार्टी “आला कमान” किस्म की नेतृत्व प्रणाली से अलग विकेन्द्रित जनतांत्रिक तरीके से अपने निर्णय करती हो, ऐसी एक पार्टी की संभावना से ख़ास तरह की सनसनी राजनीतिक हवा में फैल गई थी। कहा गया कि यह ऐसी पार्टी होगी जिसमें बुद्धिजीवी भी अपनी भूमिका निभा पाएँगे और अलग-अलग किस्म के पेशेवर (प्रोफ़ेशनल) लोग भी।
‘आप’ के गठन से सामाजिक आंदोलनों से, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन से लेकर सूचना के अधिकार आंदोलन के सदस्य, छोटे-मोटे दूसरे आंदोलनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उत्साहित हो उठे कि अब राजनीति को भीतर जाकर सकारात्मक दिशा में प्रभावित किया जा सकता है। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि इनमें से हरेक का 'आप' को लेकर भ्रम टूट गया। इन उम्मीदों के साथ 'आप' के साथ राजनीति का तजुर्बा करने गए ढेर सारे लोग टूटे हुए दिल लेकर बाहर आए। एकाध ने नया राजनीतिक प्रयोग करने की भी ठानी। लेकिन अब तक इनमें से ज़्यादातर ने ईमानदारी से यह नहीं बताया कि आख़िर उनका मोह भंग हुआ कैसे और क्योंकर! मानो यह कोई निजी प्रेम संबंध था जिसमें कोई पक्ष किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। संभव है, इसे सार्वजनिक न करने का एक कारण यह भी रहा हो कि इससे खुद उनके राजनीतिक विवेक पर सवाल उठते।
आत्म स्वीकृति और आत्मालोचना भारतीय गुण नहीं हैं। गाँधी की आत्मकथा इसीलिए अपवाद है। वह सत्य के साथ उनके प्रयोगों की कथा है। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम अपने किसी क़दम को प्रयोग कहकर छोटा करना नहीं चाहते। हम यह नहीं चाहते कि यह माना जाए कि यह भी संभव है कि हम एक समय पूरा सच न देख पाएं और न समझ पाएं।
सच न बोलने या उसमें अपनी भूमिका के कारण खुद अपनी छवि बिगड़ने के ख़तरे से जयप्रकाश आंदोलन का पूरा सच भी अब तक सामने नहीं आ पाया है। उसी तरह, जिसे अन्ना आंदोलन कहा गया, जो वास्तव में पूरी तरह अरविन्द केजरीवाल का आंदोलन था, उसका भी सच्चा वृत्तांत सामने नहीं आया है। निजी बातचीत में फुसफुसाहट की तरह टुकड़े-टुकड़े में कुछ रहस्यों की चर्चा की जाती है लेकिन अब तक हम यह नहीं समझ पाए हैं कि उस “नए”, “रैडिकल”, पुरानी राजनीति को चुनौती देनेवाले आंदोलन में कितनी प्रकार की पारंपरिक राजनीतिक शक्तियों की रुचि थी।
“नैतिक” राजनीति का दावा छोड़ा!
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के गर्भ से निकली 'आप' ने “नैतिक” राजनीति का दावा जल्दी ही छोड़ दिया। 'आप' के गठन पर आंदोलन से जुड़े कई लोगों को ऐतराज था। पार्टी चुनावी होगी, यह समझने के बाद संसदीय राजनीति के भीतर उसी के तर्कों से उसे सुधारने के अभियान की पार्टी के रूप में 'आप' का स्वागत हुआ। यह दिखलाई पड़ा कि हालाँकि देश के तकरीबन हर हिस्से में इसे लेकर दिलचस्पी थी लेकिन इसने दिल्ली और पंजाब में चुनावी पार्टी के रूप में जगह बनाई, बाक़ी राज्यों ने इसे खास तरजीह न दी। वहाँ पारंपरिक राजनीतिक अभिजन का कब्ज़ा बना रहा।
रिकॉर्डतोड़ थी 2015 में मिली जीत
'आप' के उभार का समय राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी के उभार का समय है। दिल्ली में 'आप' की केंद्र में कांग्रेस के रहते हुई जीत जितनी चमत्कारिक थी उससे कहीं ज्यादा बाद में बीजेपी के सत्तासीन होने के बाद हासिल की गई रिकॉर्डतोड़ जीत थी। मुझे अब तक 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले योगेंद्र यादव से सीटों की संख्या के अनुमान को लेकर हुई बातचीत याद है। उन्होंने हँसते हुए कहा था कि ख़तरा हमारे 60 सीटों से ऊपर जाने का है। 'आप' ने 67 सीटें हासिल कीं थीं! यह जीत इसलिए ग़ैरमामूली थी कि यह राष्ट्रीय पटल पर नरेंद्र मोदी के चक्रवर्तीनुमा अवतार के आतंक के बीच हासिल की गई थी।
जो लोग 2020 के चुनाव अभियान में बीजेपी द्वारा भरे गए ज़हर के असर से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वे 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा किये गये विषैले प्रचार को भूल गए लगते हैं। इस बार गृह मंत्री ने वही किया है जो तब प्रधानमंत्री कर रहे थे।
अरविंद केजरीवाल को इस बार आतंकवादी, पाकिस्तानी प्रवक्ता, आदि कहा गया, तब खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें ए.के.- 47 कहकर आतंकवादी बताया था। फिर भी दिल्ली की जनता ने ए.के. का हाथ थाम लिया। नरेंद्र मोदी के एक वोटर, मेरे एक परिचित ने तब कहा था: दिल्ली की जनता ने वह थप्पड़ लगाया है कि पूरे देश में इसकी गूँज रहेगी!
मीडिया ने बनाया केजरीवाल का मजाक
यह भी कहना होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त के अरविन्द मीडिया के जितने दुलारे थे, वे बीजेपी को हराकर जब सत्ता में आए तो उसी मीडिया ने उनकी खिल्ली उड़ाने और उन्हें हर तरह से लांछित करने में कसर नहीं छोड़ी। अरविंद की खाँसी तक को लेकर फूहड़ और क्रूर चुटकुले और मज़ाक का कीचड़ उछाला जाता रहा। यानी अरविंद की छवि को ध्वस्त कर देने की मुहिम-सी चल गई। सत्तासीन 'आप' को तबाह करने में केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के माध्यम से हर रास्ता अपनाया। उस हमले के सामने टिक जाना ही चमत्कार था।
रोहित वेमुला और कन्हैया प्रकरण
पांच साल के 'आप' के कार्यकाल को एक तरह से बाधा दौड़ ही कहना होगा। 'आप' को हमेशा एक नई बाधा का सामना करना था। यह बीजेपी के राष्ट्रीय चढ़ाव का वक्त था। उससे अधिक उसके द्वारा आविष्कृत राष्ट्रवादी राजनीति के उभार का। इसी बीच रोहित वेमुला ने आत्म हत्या की और इसी समय जवाहरलाल विश्वविद्यालय (जेएनयू) पर हमला शुरू हुआ। हिन्दुओं का राजनीतिक दिमाग बदल रहा था। रोहित या कन्हैया के साथ खड़ा होना जोख़िम भरा था।
याद करें कि राहुल गांधी के जेएनयू जाकर छात्रों से एकजुटता दिखाने के कारण उनपर किस तरह का हमला हुआ। उस बीच 'आप' ने जेएनयू के छात्रों का साथ दिया। वह साथ बाद तक जारी रहा और दिल्ली सरकार ने कन्हैया और दूसरे छात्रों पर राजद्रोह का मुक़दमा चलाने की अपनी ओर से इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसी तरह दिल्ली के क़रीब दादरी इलाक़े में घर से खींच कर हिंदू भीड़ के द्वारा मार डाले गए इखलाक़ के परिजन से भी मिलने का ख़तरा अरविन्द केजरीवाल ने उठाया। याद करना चाहिए कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने इखलाक़ के घर जाने से रोका भी था।
ये सांकेतिक कदम हैं लेकिन इनका आशय गहरा है। मुसलमानों या जेएनयू से सहानुभूति रखने का अर्थ वर्तमान समय में हिंदुओं की नाराजगी मोल लेना है। आम तौर पर हिंदू मन इतना संकुचित हो चुका है कि उसमें अपने पड़ोसियों के लिए हमदर्दी जगाना नामुमकिन है। यही हिंदू एक औसत वोटर भी है। इसके राजनीतिक भावनात्मक जगत को छेड़े बिना इससे वोट कैसे लिया जाए?
यह भी स्वीकार करना चाहिए कि अरविन्द केजरीवाल ने नागरिकता क़ानून में संशोधन और नागरिकता के रजिस्टर को गैरज़रूरी बताया था। इनके ख़िलाफ़ जब मुसलमानों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू किये तो शुरुआत में यह कहा गया कि हर किसी को विरोध का अधिकार है लेकिन बाद में 'आप' ने इन विरोध-प्रदर्शनों से दूरी बनाये रखी। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने ‘आप’ को इन विरोध-प्रदर्शनों के लिये जिम्मेदार ठहराया और केजरीवाल को आतंकवादी कहा।
यह चुनौती सिर्फ 'आप' के सामने हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता तो कई बार निराशा जाहिर कर चुके हैं कि उसे मुसलमानपरस्त पार्टी कहकर हिंदुओं के मन में उसके लिए हमेशा के लिए दुराव पैदा कर दिया गया है। इसलिए 'आप' से आक्रामक धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद रखना कितना उचित है?
जिस शुचिता के नारे की पतवार के सहारे 'आप' ने अपनी नैया खेना शुरू किया था, वह सीट देने, राज्य सभा के लिए उम्मीदवार चुनने और बाक़ी सारे फैसलों में टूट कर बह गई मालूम पड़ती है। पार्टी में जनतांत्रिकता की मांग भी बेकार ही है। लेकिन पार्टी के पैरोकारों का कहना है कि उसकी आलोचना न की जाए और वह है, बस इसे गनीमत माना जाए।
तो फिर ‘आप’ की राजनीति कितनी ‘नई’ रह गई है? क्या उससे एकमुश्त धर्मनिरपेक्षता की जगह किस्तवार धर्मनिरपेक्षता की आशा की जाए? क्यों उसी से आत्मघाती वैचारिकता की मांग की जाए? ये सारे सवाल उठ रहे हैं।

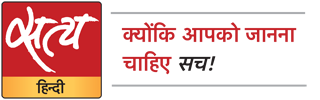





























अपनी राय बतायें