29 अप्रैल को जहाँ मतदान होनेवाला है, वहाँ प्रचार बंद हो गया। रात एक मित्र का फ़ोन आया। दूर अमेरिका से। पहला सवाल था, कन्हैयाजी जीत तो रहे हैं न? पूछनेवाले भूमिहार न थे। हिंदू भी नहीं थे। पहले भी उनका फ़ोन आता रहा था। उसी तरह भारत के दूसरे शहरों से, पुणे, देवास, रायगढ़, भोपाल, लखनऊ या और भी शहरों से, इसी उत्सुक प्रश्न के साथ। दूसरे देशों से भी इस सवाल के साथ कि कैसे कन्हैया की मदद की जा सकती है!
दिल्ली से अपने कामों से छुट्टी लेकर लोगों को बेगूसराय जाते देखा। अमूमन लोग छुट्टियाँ बचा-बचा कर ख़र्च करते हैं। लेकिन कन्हैया के लिए प्रचार करने को छात्र, शिक्षक, प्रकाशक, संपादक बेगूसराय जाते देखे गए। इनमें से कोई-कोई ही कन्हैया से परिचित हो। लेकिन सब ऐसे गए जैसे बेगूसराय में उनका कुछ बहुत क़ीमती दाँव पर लगा हो। या जैसे वहाँ कोई यज्ञ हो रहा हो, जिसमें उनकी आहुति अनिवार्य थी। पवित्रता के भाव के लिए अब तक हमारे पास धार्मिक रूपक ही हैं, पिछला वाक्य लिखने के बाद मैंने सोचा। लेकिन कन्हैया के चुनाव प्रचार में लोगों ने इसी भावना से हिस्सा लिया जैसे ऐसा न करने से वे किसी पुण्य से वंचित रह जाएँगे।
यह एक प्रकार की तीर्थयात्रा थी। जियारत। कभी अपने दोस्तों, परिजनों से बात हो तो कह सकें कि हमने अवसर नहीं गँवाया। प्रायः सुना है कहते कि जब भोलेबाबा का बुलावा आयेगा, जाएँगे। कुछ वैसा ही भाव। यह एक बुलावा था और सैकड़ों लोगों ने इसका उत्तर दिया। जितने गए, उनसे कई गुना ज़्यादा मनमसोस कर रह गए। लेकिन लगातार अपनी दुआएँ कन्हैया को भेजते रहे।
चाहिए तो कन्हैया को अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के वोट, और इतने कि वह जीत सके, लेकिन यह जो उन्हें मिला है, यह शायद भारत के किसी चुनाव में किसी राजनेता को नसीब न हुआ होगा। किसी राजनेता ने लोगों के मन में इतना स्नेह, प्रेम और आशा न जगाई होगी।
कन्हैया का योगदान इस चुनाव में यही है, इस उदात्त भाव का सृजन।
फिर भी हमारे मुल्क़ की बदनसीबी कि ढेर सारे लोग हैं जिन्हें यह बिनमाँगा प्यार कन्हैया पर न्योछावर होते देख कलेजे पर साँप लोट रहा है। उन्हें इसमें एक योजना, एक षड्यंत्र दीख रहा है। उनके लिए यक़ीन करना असंभव है कि ऐसा अनायोजित समर्थन किसी राजनेता को मिल सकता है जिसमें बदले में कोई चाह न हो। क्योंकि विद्वानों ने भारतीय जनतंत्र में नेता और जनता के रिश्ते को लेन-देन का संबंध बताया है। यानी लोग चुनाव में उसे चुनते हैं जो उनका कोई न कोई काम कराने में मदद करे। लेकिन बाहरवालों के बारे में यह बात सही नहीं। उनकी तो शायद फिर कन्हैया से भेंट भी न हो। कन्हैया के अभियान में उनका यह नि:स्वार्थ निवेश आज की आम जनतांत्रिक समझ के व्याकरण के सहारे नहीं समझा जा सकता।
जनतंत्र की मज़बूती का स्वार्थ
यह निवेश लेकिन उतना भी नि:स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ यह है कि भारत में जनतंत्र मज़बूत हो। वह कुछ मूल्यों के आधार पर ही हो सकता है। वे मूल्य साधारण लगते हैं, लेकिन हासिल करना वास्तविकता में उन्हें इतना आसान नहीं। आज़ादी, बराबरी, इन्साफ़ के मूल्य एक ऐसे समाज में जहाँ जन्म कहाँ हुआ, इससे आपकी पहचान और आपके अधिकार तय होते हों, स्वाभाविक नहीं। बहुत कम राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन मूल्यों की शिक्षा को अपना कर्तव्य माना है।
कन्हैया ने पिछले 3 वर्षों में इन्हीं मूल्यों की बात की है। इसलिए उनका विरोध भी हुआ है। लेकिन देश के एक बड़े हिस्से ने उन्हें सुनना चाहा। बहुत दिनों के बाद एक भाषा सुनाई पड़ी जो विभाजनकारी न थी, जो समाज के किसी तबक़े को दुश्मन नहीं ठहरा रही थी, जो इन मूल्यों के लिए किसी समुदाय के बलिदान की बात न करके एक बड़ी एकजुटता का आह्वान कर रही थी। इसीलिए इस ताज़ा ज़ुबान को लोगों ने अपने कानों की कटोरियों में अमृत की तरह भरा। बिना किसी पार्टी के आधार के कन्हैया का अपना जनाधार देश में और बाहर भी तैयार हुआ। उनमें से कुछ बेगूसराय पहुँचे।
बेगूसराय चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं ने इसे कुछ कौतूहल से देखा। कुछ अविश्वास से क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं। एक ने बताया कि विरोधभाव भी था कि क्या अब बाहरवाले हमें बताएँगे कि किसे चुनना है!
बेगूसराय के मतदाताओं में भी आंतरिक आलोड़न हुआ। चुनावी तर्क से कन्हैया को उसकी जाति के मतदाताओं का समर्थन मिलना चाहिए था। एक मुसलमान उम्मीदवार हैं वहाँ तो क़ायदे से उन्हें क्षेत्र के मुसलमानों का समर्थन मिलना ही चाहिए। लेकिन उनमें से कई कन्हैया को वोट देने जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने आम चुनावी तर्क को नकारा है। लेकिन क्या यही बात उन लोगों के बारे में कही जा सकती है जो ख़ुद को कन्हैया की जाति का कहते हैं? जो सूचना है, उसके मुताबिक़ उनमें से ज़्यादातर शायद कन्हैया को न चुनें! वे एक दूसरे व्यक्ति को पसंद करते हैं जो मुसलमान विरोधी घृणा का प्रचारक है। इसका अर्थ यह है कि इस जाति के लोगों को उन मूल्यों की आवश्यकता नहीं जिनकी बात कन्हैया जैसे लोग कर रहे हैं। इसके मायने यही हैं कि इस जाति के लिए किसी बड़ी जनतांत्रिक एकजुटता की कोई ज़रूरत नहीं है।
मुसलमान अपने दायरे से बाहर जाने का जोख़िम उठा रहे हैं। वे किसी और को अपना बना रहे हैं। लेकिन क्या कन्हैया के तथाकथित स्वजातीय ऐसा करना चाहते हैं? क्या वे अपने दायरे की सुरक्षा या असुरक्षा से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या वे सिर्फ़ भूमिहार और हिंदू बने रहेंगे या इन पहचानों में इज़ाफा करेंगे जिससे उनकी भारतीय नागरिकता का सबूत मिल सके?
बेगूसराय में बाहर से गए लोग यह देखकर लौट रहे हैं कि कन्हैया को उन्हीं का समर्थन नहीं मिले शायद जिन्हें पारंपरिक तौर पर अपना जन कहा जाता है।
हर चुनाव नागरिकता के निर्माण का एक मौक़ा होता है। परीक्षा भी। इस बार बेगूसराय के इम्तिहान में कौन पास होता है, यह देखना है। कन्हैया चुनाव हार जाने के बाद भी इसलिए विजेता होंगे कि उन्होंने एक व्यापक बंधुत्व की संभावना में लोगों का यक़ीन जगाया है। लेकिन अगर उनके अपने लोगों ने उन्हें नहीं चुना तो फिर ख़ुद के संकरेपन से निकलने का एक अवसर वे खो देंगे।

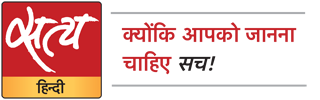





























अपनी राय बतायें