(...गतांक से आगे)
जहाँ तक केरल का सवाल है, 2018 में लेफ़्ट सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध करने वाले किसानों के टेंट माकपा कार्यकर्ताओं ने जला दिए जिसके विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ और जिसके नतीजे 2019 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिल गए। लंबे समय से लेफ़्ट केरल में अपना कोई स्थाई आधार नहीं बना सके और अब एंटी इनकम्बेंसी साफ़ दिखायी पड़ रहा है।
(2) ताक़तवर हो जाने के बावजूद लेफ़्ट ने न जाने क्यों कभी अपने दम पर ताल ठोंकने की हिम्मत नहीं जुटाई? क्यों वे अन्य 'बुर्ज़ुआ' पार्टियों के पिछलग्गू बने अपने कार्यकर्ता और प्रकारांतर से आम जनता को अपने 'शत्रु नंबर 1 और शत्रु नंबर 2 की परिभाषाएँ देने में ही उलझे रहे। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक वे कभी नेहरू और पटेल में तो कभी कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (ओ) में, कभी इंदिरा गाँधी और जयप्रकाश में तो कभी जनता पार्टी और कांग्रेस (आर) में, कभी राजीव गाँधी और विश्वनाथ प्रताप में तो कभी पीवी नरसिंहराव के नेतृत्व वाली कांग्रेस और अटलबिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी में और अब नरेंद्र मोदी और सोनिया गाँधी में 'मुख्य शत्रु' और 'प्रधान अंतर्विरोध' की तलाश करते रहे। उनके उलझाव पूर्ण क़दमों के नतीजों ने न सिर्फ़ उनके काडर को भ्रमित किया बल्कि आम जनता में भी उसका दिग्भ्रमित सन्देश गया जिसका खामियाज़ा उन्हीं को उठाना पड़ा।
ज़्यादा पुराने इतिहास में न जाएँ, अगर 70 के दशक से ही कहानी शुरू करें तो हम पाते हैं कि तब, जबकि आर्थिक-राजनीतिक संकट अपने चरम पर था और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ गुजरात में छात्रों-युवाओं का व्यापक आंदोलन चल रहा था, वामपंथी उससे कटे रहे। आगे चलकर जब यह आंदोलन बिहार तक पहुँचा और जेपी ने इसका नेतृत्व संभाला तो माकपा ने इस दलील के साथ कि ‘इसमें दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी (जनसंघ, कांग्रेस (ओ) और एबीवीपी आदि) शामिल हैं’ उसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। भाकपा उसके विरोध में खड़ी हो गयी।
आपातकाल का भाकपा ने समर्थन किया और माकपा उस पूरे दौर में 'निहुरे-निहुरे (झुक-झुक के) ऊँट चराती' रही। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को मिली भारी-भरकम जीत के बाद माकपा उसके पक्ष में आ गई। काडर पूछता रह गया कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी (जनसंघ) तो इस सरकार में भी शामिल है, फिर उनको सपोर्ट कैसा?
'ऑब्जेक्टिव' और 'सब्जेक्टिव' हालातों के उनके अपने अध्ययन इतने लचर और कमज़ोर थे और आत्मविश्वास की उनमें इतनी कमी थी कि 1977 में हुए विधानसभा चुनावों में माकपा जनता पार्टी से बंगाल में 48% - 52% सीटों के तालमेल की याचिका करती रही और जनता पार्टी के बंगाल प्रमुख पीसी सेन उन्हें 25% से ज़्यादा सीटों की 'भीख' के लिए तैयार नहीं हुए। तब मजबूरन (!) प्रमोद दास गुप्त और ज्योति बसु अपना अलग वाम मोर्चा बनाकर (जिसमें भाकपा शामिल नहीं थी) डरते-डरते मैदान में उतरे और 294 में से 231 सीटों (78.5%) पर शानदार जीत हासिल की। जनता पार्टी ने 289 उम्मीदवार खड़े किए थे, वह सिर्फ़ 29 पर ही जीत सकी।
स्वतंत्र रूप से 63 सीटों पर लड़ी भाकपा सिर्फ़ 2 सीटें जीत सकी। कई महीने बाद वह वाम मोर्चा में शामिल हुई और तभी से कम्युनिस्ट पार्टियों में बड़े और छोटे भाई की भूमिका के विवाद पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लग गया।
(3) आत्मविश्वास में कमी का एक और बड़ा ख़ामियाज़ा कम्युनिस्टों ने साम्प्रदायिकता विरोधी आंदोलन के कमज़ोर हो जाने और प्रकारांतर से भाजपा के सुदृढ़ होते जाने की क़ीमत पर चुकाया। आज़ादी के समय से ही कम्युनिस्ट अकेली ऐसी शक्ति थे जो ‘24 कैरेट के धर्मनिरपेक्ष’ माने जाते थे। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, सन 47 से पहले भी उसके भीतर धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक तत्वों का सामूहिक वास था और 47 के बाद भी। 60 और 70 के दशक में जिन-जिन राज्यों में हिंदू-मुसलिम दंगे हुए, वहाँ-वहाँ कांग्रेस की हुक़ूमतें ही थीं। 80 के दशक में जिस तरह पंजाब और कश्मीर में साम्प्रदायिकता फैली, उसमें कांग्रेस, उसकी नेता इंदिरा गाँधी और संजय गाँधी की भूमिका भी कम विवादास्पद नहीं मानी जाती थी। अंततः श्रीमती गाँधी उसी सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुईं, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। उनकी हत्या के बाद देश में बड़े पैमाने पर सिखों का क़त्लेआम और हिंदू साम्प्रदायिकता का जैसा ज्वार आया, उसने सन 47 की यादें ताज़ा कर दीं। श्रीमती गाँधी की हत्या से लेकर अगले चुनाव तक देश में हिंसा के जैसे बलवले फूट रहे थे, उसमें कांग्रेस और 'संघ' परिवार दोनों की सामूहिक मिलीभगत मानी जाती थी। नई पीढ़ी को सुनकर आश्चर्य होगा कि कांग्रेस को सन 84 के लोकसभा चुनाव जिताने में 'संघ' परिवार ने भी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया था बेशक उसकी अपनी पार्टी (बीजेपी) को 2 ही सीटें क्यों न मिली हों। इस पूरे दौर में लेफ़्ट पार्टियों ने एक बार भी आगे बढ़कर ‘सांप्रदायिक’ कांग्रेस के ख़िलाफ़ मोर्चा नहीं संभाला। पंजाब में तो वह 'आतंकवाद से निबटने' के नारे के साथ कांग्रेस और राजसत्ता की मशीनरी की हमजोली बनी रही थी।

80 के दशक का बाबरी मसजिद का ‘ताला खोल’ काण्ड, शाहबानों प्रकरण, दूरदर्शन पर 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे धारावाहिकों के प्रसारण के विरूद्ध न तो लेफ़्ट ने एक बार भी अपनी ज़बान खोली और न उन्होंने कांग्रेस से अलग हटकर अपने कन्धों पर साम्प्रदायिकता विरोधी मोर्चा बनाया। आगे चलकर जनता दल शासन काल में, आडवाणी के रथ की ज़ब्ती के बाद जब बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता सरकार से अपना हाथ खींचा तो वामपंथियों ने उसे बचाने में अपनी हथेली लगा दी। उन्होंने साम्प्रदायिकता विरोधी अलख जगाई लेकिन मुलायम और लालू की पूँछ पकड़ कर। उन लोगों के ‘धर्मनिरपेक्ष हित’ विधान सभा की सीटों के तालमेल से ज़्यादा जुड़े थे, साम्प्रदायिकता विरोध की अगन से कम। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव की इस ‘संसदीय धर्मनिरपेक्षता’ ने 'संघ' परिवार को 'मुसलिम सन्तुष्टिकरण' का नारा लगाकर बहुसंख्य हिंदुओं को साम्प्रदायिकता के जाल में फँस जाने को मजबूर कर दिया।
यहाँ यदि लेफ़्ट एक सुदृढ़ धर्मनिरपेक्षता का परचम ख़ुद उठाते और पूरे साम्प्रदायिकता विरोधी आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करते तो बात दूसरी होती। अपने शासन वाले तीनों राज्यों में उन्होंने न तो अल्पसंख्यकों को विकसित किया न महिलाओं को।
संसद में भी उनके नेतृत्व की डोर इनमें से किसी के हाथ में नहीं थी। उस नरसिंहराव सरकार के उत्तरार्ध के ढाई साल के प्राणदाता लेफ़्ट बने जिसके पूर्वार्द्ध के ढाई साल का ज़िम्मा बीजेपी ने निभाया था। यह वही नरसिंहराव सरकार थी जो बाबरी मसजिद के ध्वंस को किंकर्तव्यमूढ़ खड़ी देखती रही थी।
लेफ़्ट ने कश्मीरियों के स्वायत्तता के सवाल को भी बगलगीर कर दिया और इस तरह 'घाटी' को इस्लामिक कठमुल्लों और हिन्दू कट्टरपंथियों के हाथों में जाने के लिए छोड़ दिया। ‘धर्मनिरपेक्षता’ के नाम पर 4 दशक तक जैसा संसदीय अवसरवाद चला, उसका फ़ायदा सांप्रदायिक तत्वों को अधिक मिला, कथित धर्मनिरपेक्ष तत्वों को कम। वामपंथी नेतृत्व के अवसर से पिछड़ गए और किंकर्तव्यमूढ़ बने देश को सांप्रदायिकता की झोली में जाता देखते रहे।
(4) बाद में जिसे 'ऐतिहासिक भूल' के तौर वामपंथियों ने स्वीकार किया, वह था अवसर आने पर भी ज्योति बसु को प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचने से रोकना।
2004 के यूपीए-1 के काल में 'मनरेगा', भोजन का अधिकार, वन का अधिकार और सूचना का अधिकार जैसे क़ानूनों को संसदीय लोकतंत्र में मील का पत्थर माना जाता है। इन अधिकारों को लागू करवाने में वाम मोर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो उस समय के यूपीए-1 को बाहर से समर्थन दे रहा था। उनके समर्थन की गारंटी था 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम।' माना जाता है कि सन 96 में यदि एचडी देवेगौड़ा की जगह ज्योति बसु प्रधानमंत्री होते तो न सिर्फ़ देश के आर्थिक-सामाजिक ढांचे में बुनियादी अंतर आता बल्कि साम्प्रदायिक ताक़तों के विनाश का भी कोई ठोस एजेंडा बन पाता लेकिन जैसी कि प्रवत्ति थी, यहाँ भी वामपंथियों का आत्मविश्वास जवाब दे गया और उन्होंने पद स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

(5) अपने ज्ञान और विवेक का लोहा मनवाने के लिए कम्युनिस्ट सारी दुनिया में मशहूर माने जाते रहे हैं। दुनिया भर की कम्युनिस्ट परंपरा के तहत 'पार्टी' में नए कार्यकर्ता को शामिल करने के साथ ही उसको ज्ञान, विवेक और वैज्ञानिक सोच से लैस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समय-समय पर होने वाली पार्टी की 'क्लास' और 'स्टडी सर्कल' में उन्हें और भी प्रशिक्षित करके तराशा जाता रहा है। सत्ता में शामिल होने से पहले भारत में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। बाद में यह औपचारिक क्रिया बन कर रह गई। सत्ता से दूर रहने वाले प्रतिबद्ध और पुराने कार्यकर्ता आने वाले युवा काडर को देख-देख कर हैरान होते हैं। उनका कहना है कि ये न मार्क्सवाद-लेनिनवाद जानते हैं न इन्हें भारतीय समाज की कोई ठोस समझ है और न इसका कोई इंतज़ाम किया जा रहा है।
उधर सत्ता में आने के बाद वामपंथी यदि चाहते तो अपने शासित राज्यों के प्राथमिक स्कूलों से कॉलेजों तक ज्ञान-विज्ञान से लेकर मार्क्सवादी शिक्षा का प्रसार कर सकते थे। ऐसा होता तो नई पीढ़ी अज्ञानता, अन्धविश्वास और सांप्रदायिकता के ज़हर में डूबने से स्वयं को बचा लेती। केरल में पुरानी परंपरा के रूप में यह कुछ-कुछ दिखाई देती है लेकिन बंगाल में इसका पूर्णतः लोप रहा।
पश्चिम बंगाल में 2011 से लुढ़कते हुए 2019 में रसातल तक पहुँच जाने के वोट शेयर के पीछे कारण बंगाली मतदाताओं का लेफ़्ट की झोली से निकल कर बीजेपी की गोद में बैठ जाना बताया जाता है। सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? वजह है ममता दीदी के ‘भ्राताओं’ का लेफ़्ट समर्थकों के प्रति हिंसक होना। टीएमसी बनाम लेफ़्ट के बीच घृणा की यह लड़ाई 21वीं सदी के पहले दशक से ही जारी थी। विज्ञान, अज्ञानता, अन्धविश्वास और धार्मिक कूपमंडूकता की परंपरागत विचारधारा से लैस मतदाता जब लेफ़्ट से नाराज़ हुए (नाराज़गी के आर्थिक-सामाजिक कारणों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है) तो उनके पास दूसरा विकल्प बीजेपी थी, वे वहाँ चले गए।
तो क्या अब यह मान लिया जाए कि ताज़ा किसान-मज़दूर आंदोलनों में पूरी शिद्दत और ताक़त के साथ शामिल लेफ़्ट अपने भूत की ग़लतियों से सबक़ हासिल करके यहाँ तक पहुँचा है?
अगर यह मान भी लिया जाए कि लेफ़्ट ने अपने भूतकाल की ग़लतियों से सबक़ लिया है तब भी आगामी विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और केरल में सरकार बना पाने की उम्मीद लगाना कारगर नहीं?
देश में आर्थिक व्यवस्था की जो दशा है उसके चलते आने वाले दिन और भी गंभीर संकट के हैं। अर्थव्यवस्था की जो हालत है उसमें बहाली का एक ही रास्ता रह जाता है वह है माँग (विशेषकर उपभोक्ता माँग) में बढ़ोतरी का। माँग में इस तरह की बढ़ोतरी महामारी में फँसी जनता के कल्याण के लिए भी ज़रूरी है और अर्थव्यवस्था के कल्याण के लिए भी। लेकिन इस 'माँग' में नई जान डालने के लिए सरकार ने न के बराबर कुछ किया है। इसके विपरीत जो सीमित बहाली हुई भी है उसके साथ अतिरिक्त मूल्य में ही बढ़ोतरी होती दिख रही है जो आने वाले दिनों में आर्थिक बहाली को जाम कर देगी। ऐसे में श्रमिक-किसान संकट बढ़ेगा और उनका स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध भी। शासन के पास इस संकट और प्रतिरोध से निबटने का एक ही रास्ता है, वह है दमन और उत्पीड़न का रास्ता। यहाँ लेफ़्ट के सामने एक बहुत बड़ी भूमिका की दरकार हो जाती है। यदि वह इसका सफलतापूर्वक मुक़ाबला कर पाने में सक्षम हो पाता है तब बंगाल और केरल के चुनाव की चुनौती उसके लिए ज़्यादा महत्व की न बचेगी।
लेफ़्ट में होने वाली इस चर्चा में हाल में शामिल हुई जिस नई शक्ति का उल्लेख करना बेहद आवश्यक है वह है भाकपा (माले) की एंट्री। बिहार के विधानसभा चुनावों में भाकपा और माकपा की तुलना में 'माले' ने जिस प्रकार अपने शानदार प्रदर्शन का जलवा बिखेरा है उसकी चर्चा सर्वत्र हुई है। यहाँ उन मुद्दों का ज़िक्र ज़रूरी है जिनके चलते ‘माले’ को यह शक्ति प्राप्त हुई, बाक़ी लेफ़्ट को नहीं। क्या ये उनकी चाणक्य नीतियों का कमाल था या कई दशकों की उनकी सुविचारित सोच और रणनीति का? क्या वे भविष्य में भी इसी समझदारी पर क़ायम रह सकेंगे या अपने वामपंथी सहोदरों की तरह भटक जायेंगे, इसे जाँचने की ज़रूरत है।

बिहार में 'माले' 70 के दशक से सक्रिय है। तब उसकी गिनती नक्सल नेता चारू मजूमदार के 'सशत्र संघर्षों और संसदीय चुनावों का बहिष्कार' लाइन के पक्षधर वाले 'अल्ट्रा लेफ़्ट' के तौर पर होती थी। 80 के दशक के अंत में पार्टी ने अपनी पुरानी लाइन बदली और ज़मीनी संघर्षों के साथ-साथ संसदीय चुनावों में भी हिस्सेदारी का फ़ैसला किया। सन 91 से उसने लोकसभा में अपना दाख़िला लिया और फिर वह बारी-बारी से बिहार विधानसभा में प्रवेश करती रही लेकिन 'सिंगल डिजिट' पार्टी के रूप में। आज ‘डबल’ डिजिट' तक पहुँचने में उसे बड़े-बड़े आर्थिक-सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ा है। माना जाता है कि इस बार उसने भोजपुर और दक्षिण बिहार में अपनी पताका लहराई जो उसके पुराने जनाधार के क्षेत्र हैं लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए उसने 2 सीटें उस सीमांचल में भी हासिल की हैं जो मुसलिम बहुल क्षेत्र है और जहाँ ओवैसी की डुगडुगी अच्छे से पिट रही थी।
'माले' ने अपने वामपंथी 'बड़े भाइयों' से इतर शुरुआत में ही यह समझ बना ली थी कि उन्हें केवल आर्थिक संघर्ष ही नहीं बल्कि सामाजिक व राजनीतिक न्याय के लिए भी सख़्ती से लड़ना होगा। यही वजह है कि दक्षिण बिहार में उसने केवल भूमि और वेतन के सवाल को ही अपने संघर्षों का मुद्दा नहीं बनाया बल्कि भोजपुर में उच्च वर्ण सामंतों द्वारा दलित महिलाओं के शोषण से शुरू करके आगे चलकर दलितों को उनके वोट के अधिकार से वंचित रहने के सवाल को अपनी लड़ाई का मुख्य आधार बनाया। इन सवालों को भाकपा और माकपा ने कभी नहीं उठाया था जबकि वहाँ भाकपा एक स्थापित पार्टी के रूप में जमी हुई थी।
एनसीआर, एनपीआर और सीएए के सवालों पर 'माले' ने अपनी लाइन स्पष्ट रखी। उन्होंने इन्हें सिर्फ़ मुसलमानों से जुड़े मसले नहीं माना अपितु पूरे उत्पीड़ित श्रमिक समुदाय के समान नागरिकता के मुद्दों के तौर पर व्याख्यायित किया।
यही वजह है कि जब कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे लोगों ने बिहार पहुँचकर 'माले' को शाहीन बाग़ की हिमायती 'इण्डिया ब्रेकिंग गैंग' कहा तो 'माले' ने शाहीन बाग़ को ‘अपने समय के समान नागरिकता के गौरवशाली आंदोलन' कहकर जवाबी हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने जनतान्त्रिक अधिकारों की पक्षधरता का आह्वान करते हुए अपनी आमसभाओं में यह घोषणा भी की कि यदि महागठबंधन की विजय हुई तो बिहार की जेलों में उमर ख़ालिद, सुधा भरद्वाज, आनंद तेलतुंबड़े, बरवरा राव और स्टेन स्वामी जैसों को अकारण निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।
भाकपा और माकपा से अलग 'माले' ने पहले तब कभी आरजेडी से चुनावी गठबंधन नहीं किया जब वे सत्ता में थी। मौजूदा महागठबंधन का हिस्सा बनने से पहले 'माले' के इस नज़रिये को समझ लेना ज़रूरी है। अब आकर उन्होंने घोषणा की कि बीजेपी के विस्तार को वैचारिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता की मदद से सख़्ती रोके जाने को पहली प्राथमिकता बनाना होगा। उन्होंने देश में विपक्ष से ग्रासरूट स्तर पर आजीविका, रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक अन्याय और समानता के लिए लड़ने का आह्वान किया।
वीडियो चर्चा में देखिए, वामपंथ का मुक़ाबला कर पाएगी बीजेपी?
बेशक़ बिहार में महागठबंधन सरकार न बना सका और 'माले' को सत्ता की भागीदारी की अग्निपरीक्षा से नहीं गुज़रना पड़ा लिहाज़ा फ़िलहाल वह उन सभी ख़तरों के भंवर में डूबने-उतराने से बच गई जिसमें उसके ‘वामपंथी भाई’ अपनी बारी आने पर फँस गए थे। लेकिन वे उन दूसरी ग़लतियों को करने से कैसे बचे रह सकेंगे जो उनके सहोदरों ने की थी और जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है? इसका निर्धारण आने वाला समय ही कर सकेगा।

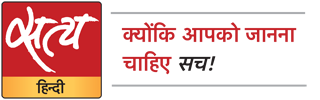














अपनी राय बतायें