“ऑश्वित्ज़ के बाद कविता लिखना बर्बरता है।” थियोडोर अडोर्नो का यह वाक्य अक्सर इस रूप में ग़लत उद्धृत किया जाता रहा है: “ऑश्वित्ज़ के बाद कविता लिखना नामुमकिन है।” दिलचस्प यह है कि यह विकृत वाक्य इतना लोकप्रिय हो गया कि ख़ुद अडोर्नो ने एक तरह से इसके लिए अपनी ज़िम्मेवारी कबूल करते हुए बाद में संशोधन किया और लिखा,
“अनंत पीड़ा को भी व्यक्त होने का उतना ही अधिकार है जितना एक यंत्रणा झेल रहे इंसान को चीखने का, इसलिए यह कहना शायद ग़लत था कि ऑश्वित्ज़ के बाद आप कविता नहीं लिख सकते।”
अडोर्नो ने लेकिन अपने मूल प्रश्न को छोड़ा नहीं। इसके बाद वह लिखते हैं, “लेकिन एक कम सांस्कृतिक प्रश्न उठाना ग़लत न होगा (और वह यह है) कि क्या ऑश्वित्ज़ के बाद जीते जाना संभव है, ख़ासकर उसके लिए जो संयोगवश बच निकला हो, जिसे क़ायदे से मार डाला जाना चाहिए था! उसके बचे रहने भर के लिए वह ठंडी उदासीनता ज़रूरी है जो बोर्जुआ आत्म का बुनियादी उसूल है, जिसके बिना कोई ऑश्वित्ज़ हो ही नहीं सकता था; यह वह अंतिम अपराध बोध है जो उससे बिंध गया है जो छोड़ दिया गया था।”
अडोर्नो स्वयं अपने बारे में लिख रहे थे। बचे रह जाने का तीखा अपराध बोध बर्तोल्त ब्रेख्त की इस छोटी कविता में इस तरह व्यक्त हुआ है,
“मैं जानता हूँ निश्चय ही, यह बस नसीब था
कि अपने इतने सारे दोस्तों के (मारे जाने के) बाद मैं बचा रह गया;
लेकिन कल रात सपने में
मैंने उन दोस्तों को मेरे बारे में कहते सुना,
‘सर्वाइवल ऑफ़ द फिटेस्ट’
और मुझे ख़ुद से नफ़रत हुई।”
प्रिमो लेवी को संगियों के चेहरे याद आते हैं, धुंधले से,
“पीछे हटो, मुझे अकेला छोड़ दो, डूब चुके लोगो
चले जाओ, मैंने किसी से कुछ लिया नहीं,
किसी के हिस्से की रोटी मैंने नहीं छीनी।
मेरी जगह कोई और नहीं मरा। कोई नहीं।
लौट जाओ अपनी धुंध में
यह मेरा कसूर नहीं कि मैं जीता हूँ और साँस लेता हूँ,
खाता, पीता, सोता और कपड़े पहनता हूँ।”
अडोर्नो इस अपराध बोध की बात कर रहे हैं उन लोगों में जिन्हें क़ायदे से ख़तम हो जाना चाहिए था लेकिन जो बचे रह गए। लेकिन क्या उनमें, जो किसी भी तर्क से मारे जानेवालों में शामिल हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे न यहूदी थे, न रोमा, न कम्युनिस्ट। क्या उनमें कभी अपराध बोध जगा? अगर हाँ तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे हुई?
याशा मूंक ने अपनी किताब “अपने ही मुल्क में अजनबी: आधुनिक जर्मनी में एक यहूदी परिवार” में इस सवाल पर विचार किया है। क्या आज के जर्मन लोगों को अपने पूर्वजों के कृत्य के लिए ज़िम्मेवार महसूस करना चाहिए और पछतावे में रहना चाहिए? लोग अपनी पहचान आख़िर कैसे बनाते हैं? आख़िर यहूदी यहूदी कैसे होता है? याशा का कहना है, “यदि अपनी कहानी ईमानदारी से सुनाने का मतलब अधिकतर श्रोताओं या दर्शकों की निगाह में आपको यहूदी बना देता है और अगर यहूदी होने का मतलब आपको सच्चे मायनों में जर्मन नहीं रहने देता तो फिर जितने दिन मैं जर्मनी में रहा मेरे परिवार के इतिहास ने मुझे यहूदी बना दिया।” यहूदी की उनकी परिभाषा सरल है, “आप यहूदी हैं, अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी यहूदी कहे जाते थे, यहूदी होने के कारण जिन्हें प्रताड़ित किया गया और और जो यहूदी की तरह मारे गए।”
यहूदी आत्म बोध तो यह है लेकिन जर्मन आत्म बोध? इसी किताब में इसको समझने के लिए अलग-अलग प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लेखक के एक जर्मन दोस्त मार्कस ने किशोरावस्था में हॉलोकास्ट पर एक डाक्यूमेंट्री देखने के बाद शर्म के मारे यहूदी धर्म ग्रहण कर लिया।
दूसरी तरफ़ अब इधर की पीढ़ी के जर्मन यह शिकायत करते हैं कि आख़िर उन्हें कितने दिनों तक पछतावे का यह बोझा ढोना पड़ेगा! इसका कभी तो अंत होना चाहिए!
हिटलर कोई अपवाद नहीं
इसीलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि जर्मनी में या यूरोप में हिटलर कोई अपवाद न था! फिर क्या ऑश्वित्ज़ का अनुमान करना इतना कठिन था? क्या जर्मनी हिटलर की अगवानी करने के लिए पहले से तैयार था? 2015 के साल पेरिस के एक कबाड़ी बाज़ार में 1924 में बनी एक ऑस्ट्रियाई मूक फ़िल्म “यहूदी के बिना एक शहर” की रील मिली। इस फ़िल्म को गुम मान लिया गया था। ध्यान रहे यह फ़िल्म यहूदियों के कत्लेआम के 20 साल पहले बनी थी। इस समय ऑस्ट्रिया में नाज़ी पार्टी पर पाबंदी थी और जर्मनी में हिटलर जेल में आत्म कथा पर काम कर रहा था। यह फ़िल्म एक ऐसे शहर की कहानी कहती है जो अपने सारे यहूदियों को निष्काषित कर देता है। बढ़ती क़ीमतों और बेरोज़गारी के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है।
एक कट्टर यहूदी पर तीन मर्द फब्तियाँ कसते हुए उसका पीछा करते हैं।
बाज़ार में एक औरत ऊँची क़ीमतों पर नाराज़ हो उठती है। वह उधर से गुज़र रहे एक यहूदी को फल चलाकर ही मारने लगती है।
आगे चांसलर के दफ्तर के बाहर भारी भीड़ विरोध करती हुई जमा हो जाती है। भीतर नेता एक सलाहकार से मशविरा करता है। “यहूदियों को बाहर करना बहुत बुरा है।” वह कहता है, “लेकिन हमें लोगों को संतुष्ट तो करना ही होगा।”
ये दृश्य क्या आज के भारत की भी याद दिलाते हैं? फ़िल्म में बाद में ऐसे दृश्य हैं जिनमें यहूदियों को शहर से निकाले जाते हुए दिखाया गया है।
क्या फ़िल्मकार ह्यूगो बैत्तौर (!) को इसका अंदाज़ था कि उनकी कल्पना के ये दृश्य 20 साल बीतते न बीतते जर्मनी, पोलैंड और दूसरे मुल्कों में असलियत में बदल जाएँगे? फ़िल्म बनाने के एक साल के बाद ही एक नाज़ी ने ह्यूगो की हत्या कर दी। बहुत हलकी सज़ा के साथ वह बरी हुआ।
ऑश्वित्ज़ एक प्रकिया की परिणति थी। क्या वह होना अवश्यम्भावी था? हिटलर ने क्या पहले से यह सोच रखा था? क्या किसी प्रक्रिया को अस्वीकार करने के लिए उसके अंतिम बिंदु की भयावहता ऑश्वित्ज़ से तुलनीय होनी चाहिए? जब तक वह न दीखे, क्या वह प्रक्रिया सह्य हो?
ऑश्वित्ज़ एक क़त्लगाह का नाम है। भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य में उसकी स्मृति है। ऑश्वित्ज़ में कैद और अनिवार्य हत्या की प्रतीक्षा कर रहे लोगों में से जो बचे रह गए थे उन्हें आज से 75 साल पहले, 27 जनवरी, 1945 को सोवियत संघ की लाल सेना ने मुक्त किया।
75 साल बाद जर्मनी और यूरोप उसी यहूदी विरोधी घृणा को फिर से पनपते देख रहा है। लेकिन ऑश्वित्ज़ एक दूसरे रूप में शायद पूरी दुनिया में है। हमारे क़रीबी श्रीलंका, म्यामार में। अभी हाल में म्यांमार की सरकार और फौज को संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने अपने यहाँ रोहिंग्या लोगों का कत्लेआम रोकने का हुक्म दिया है। लेकिन हम ऑश्वित्ज़ मुक्ति के इस 75वें साल में क्यों न अपने देश को ध्यान से देखें। क्या हमारे दिमाग़ों में ऑश्वित्ज़ बन रहे हैं? भारत और ऑश्वित्ज़ में कितना फासला बचा है?

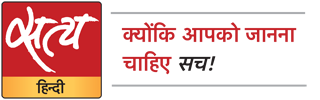





























अपनी राय बतायें