सोचा था... किसी को श्रद्धांजलि नहीं दूँगी। बहुत हो गया। पिछले दिनों इतने क़रीबी गुजरे कि दामन ख़ाली हो गया। आँखें पथरा गई हैं। रोते हैं मगर आँसू नहीं, सूखे पत्ते झरते हैं।
हर सुबह अब जागने से डर लगने लगा है। ख़बर जैसे इंतज़ार में बैठी रहती है। कोई सुबह ख़ाली नहीं। मृत्यु को रोज़ हमारे लोग चाहिए।
घनिष्ठ मित्र अरुण पांडेय चले गए।
पत्रकार साथी अशोक प्रियदर्शी चुपचाप चले गए।
आज सुबह मेरे अभिभावक -मित्र पत्रकार शेष नारायण सिंह चले गए। कल उनके प्लाज़्मा का इंतज़ाम भी हो गया था। हम आश्वस्त थे कि अब ख़तरा टल गया है, वे ठीक हो जाएँगे। अस्पताल से बाहर आकर अपने ठेठ देशी अंदाज़ में कहेंगे- ‘ई ससुर, कोरोनवा हमको काहे धर लिया... हम ससुरे को पछाड़ दिए।’
इसी अंदाज में वे बातें करते थे। हमेशा परिहास के मूड में और अपने देशी अंदाज में। इतना पढ़ा लिखा इंसान हमेशा अपने को देसी अंदाज में रखता था। उनसे गाँव -घर की ख़ुशबू आती थी। मेरे लिए हमेशा अभिभावक की तरह रहे। पिछली यात्रा हमने शिमला की साथ की थी। साथ गए और लौटे।
साथ तो हमारा नब्बे के दशक से था। जब वो राष्ट्रीय सहारा अख़बार संभाल रहे थे। मुझे बुला कर कला दीर्घा कॉलम लिखने को कहा। जो दो साल तक मैंने वहाँ लिखा। इस कॉलम की भी कहानी है। वहाँ उनकी टीम मुझे ये कॉलम देने से हिचकिचा रही थी। शेष जी ने मुझसे कला पर एक छोटा लेख लिखवाया और अपनी टीम के सामने रख दी। सबने पढ़ा और फिर सब तैयार हो गए। एक नयी पत्रकार से एक बड़ा अख़बार इतना महत्वपूर्ण कॉलम लिखवा रहा था... सब हैरान थे। मैं खुद यक़ीन नहीं कर पा रही थी। शेष जी को मुझ पर जाने कैसे यक़ीन हुआ। यह यक़ीन जीवन भर बरकरार रहा।
यही नहीं... बाद में जब मैंने एक अख़बार ज्वाइन किया, संसद कवर करने लगी तो वहाँ रोज़ उनसे मुलाक़ात होती। हम साथ ही घूमते और वहाँ कैंटीन में खाते। एक दिन उनके पास तीस रुपये कम पड़ गए। मैंने तीस रुपये दिए- हाथ में लेते हुए बोले - भाई लोगों, गीता से मैंने अपने तीस रुपये उधार के वापस लिए, बचे 70। बोलिएगा, जल्दी वापस कर दे। वहाँ कुछ पत्रकार बैठे थे। सब हँसने लगे। मैं खुद अकबका गई। ये देखो... उल्टी बात कर रहे।
इसके बाद हर रोज़ या जब कभी कहीं मिलते तो छेड़ते - गीता, तुम मेरे 70 रुपये कब वापस कर रही हो? करोगी कि नहीं। हम सबको बोल देंगे, देखिए भाई लोग, ये मोहतरमा मेरा 70 रुपये उधार वापस नहीं कर रही।
मैं कहती- आप मेरा 30 रुपया पहले दीजिए, फिर देती हूँ।
यह घटना इतनी रोचक हो चली कि जहाँ भी मिलते- माहौल में तीस और सत्तर का चुटकुला चलता। कुछ लोग सीरियसली उधार समझते। फिर शेष जी मामला बताते। मने हँस हँस के सबका बुरा हाल।
अभी ये लिखते हुए मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है... और हम दोनों की रट भी... तीस दीजिए, नहीं पहले तुम मेरा 70 वापस करो...
यह उधार हम दोनों का एक दूसरे पर रह गया।
शेष जी...
जब वहाँ मिलेंगे... फिर से ठहाका लगा कर उस लोक को भी कंफ्यूज्ड कर दीजिएगा। वहाँ भी आपके जाने से माहौल देसी और मज़ेदार हो गया होगा। आपकी आत्मीयता वहाँ छलक रही होगी।
अनेक स्मृतियाँ हैं आपकी। क्या क्या लिखूँ? कितने मंचों पर साथ रहा। आप भरोसे की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मुझे अहसास दिलाते रहे कि मैं बहुत गुणी हूँ।
याद है-
प्रेस क्लब में एक पत्रकार मित्र ने पूछा - कहाँ ग़ायब हो गीता?
आपने कहा- ‘हमारी लड़की साहित्य में बहुत अच्छा कर रही है। यहाँ धाक जमा कर हमने वहाँ काम पर लगा दिया। इसको पढ़िए तो आप लोग...!’
उस दिन दीवाली मेला था… आपने दीवानों की तरह भाभी और बेटियों के लिए साड़ियाँ ख़रीदीं, जोया के स्टॉल से। मेरी पसंद आपको इतनी पसंद आई कि बाद में भी जोया के यहाँ से आपने वो कलाकारी वाली साड़ियाँ मँगवाईं।
मैं हैरान। कितना ख़रीद रहे।
‘अरे गीता... तुम्हारी भाभी को बहुत पसंद आई तुम्हारी पसंद। तुम तो मुसीबत करवा दी हो... और मँगवाने का आदेश हुआ है…’
भाभी के साथ शिमला जाते -आते हम इस शॉपिंग पर बातें करते और हँसते।
वो आपकी कलाप्रियता पर बात कर रही थीं।
क्या क्या लिखूँ...
अपनापन की कोई तस्वीर बनती तो आपका चेहरा बनता।
आप मेरे जीवन के देसी राग थे... बजते थे तो पराया देश अपना गाँव लगने लगता था। हम सब छोड़ कर आए थे, जिन लोगों ने अनजान दुनिया को हमारे लायक बनाया... उनमें एक आप थे।
विदा नहीं दूँगी मैं.... उठिए और ठहाके लगाइए...।

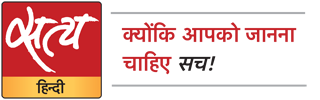
































अपनी राय बतायें